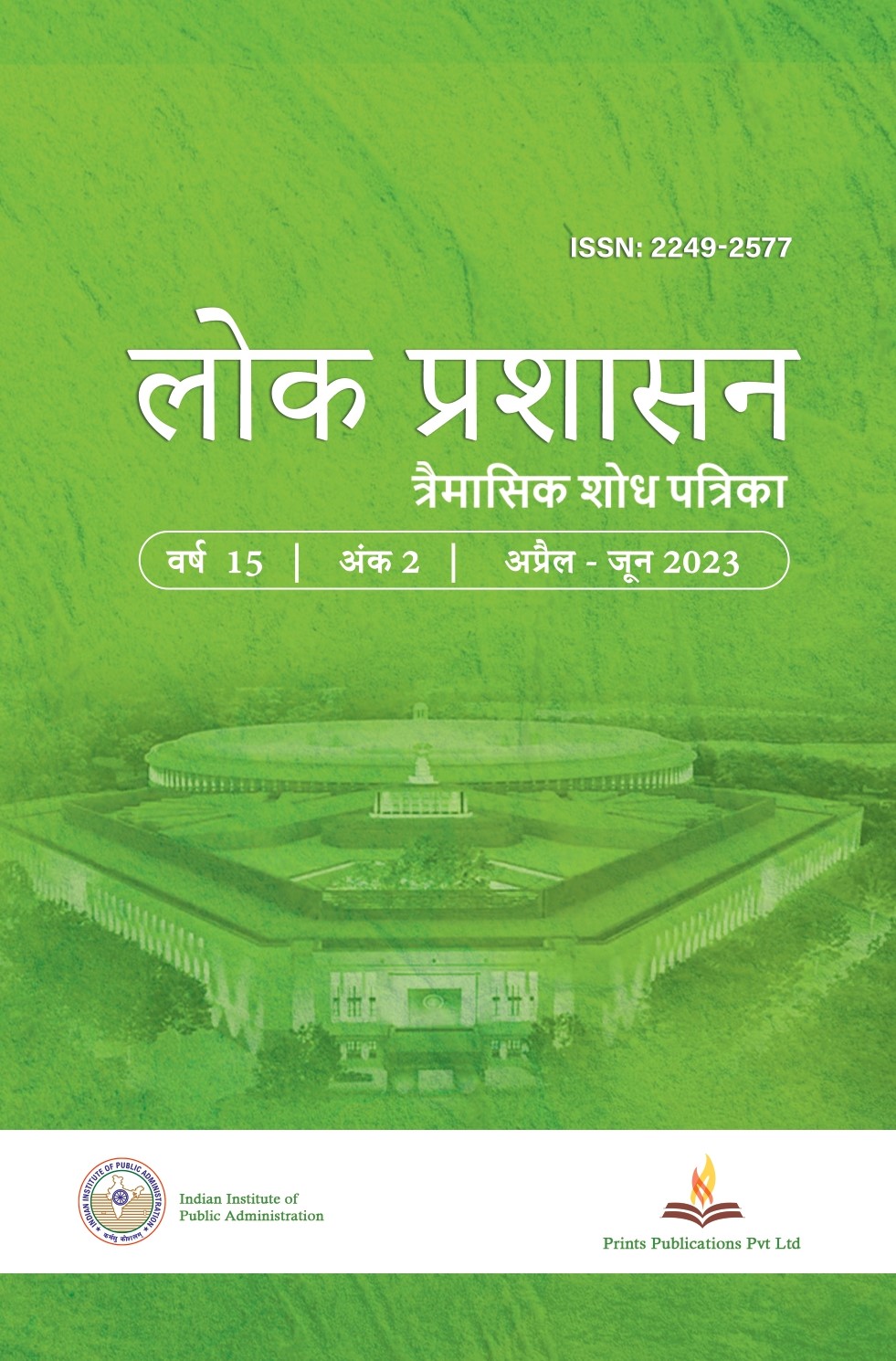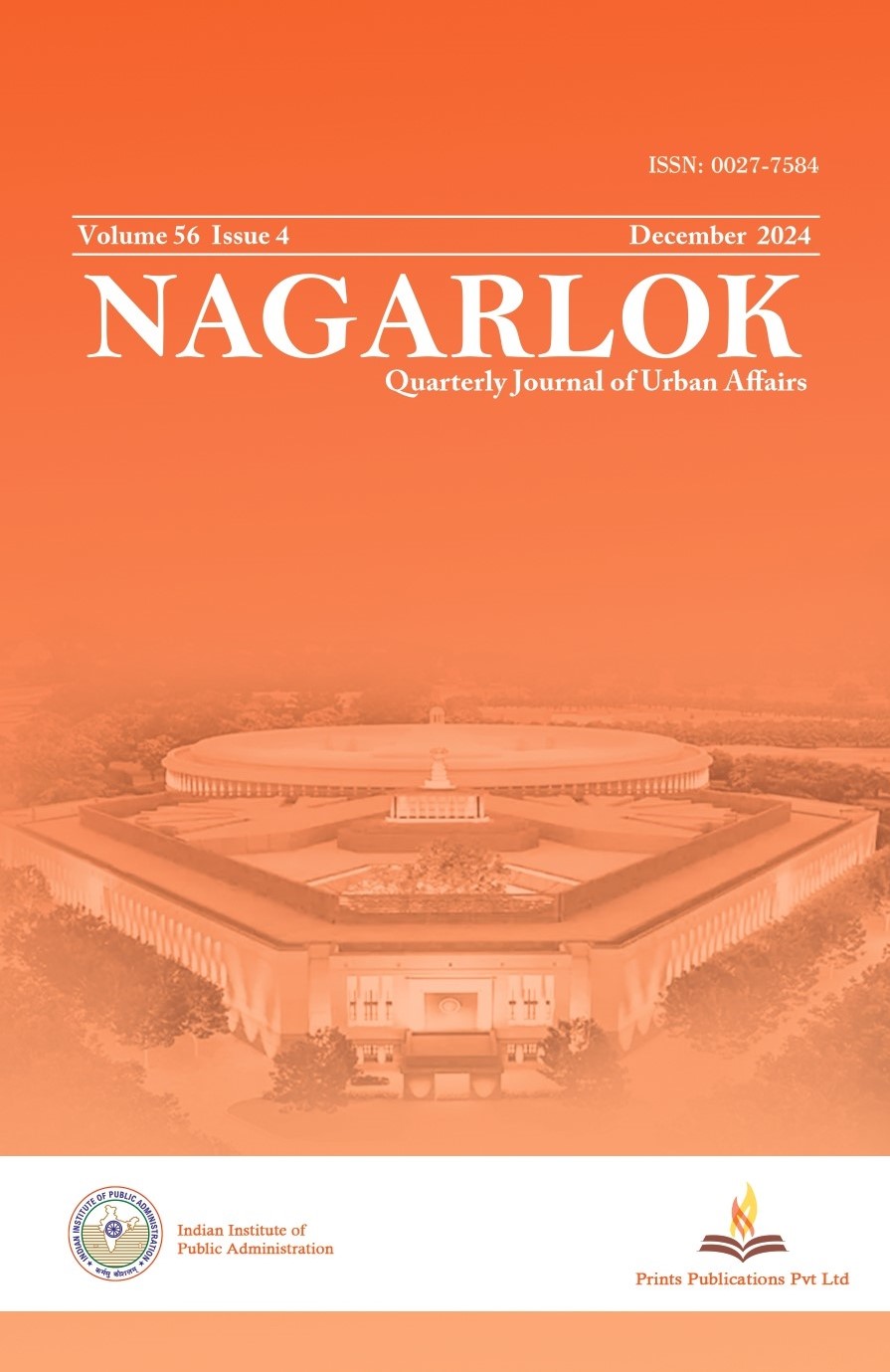लोक प्रशासन - A UGC-CARE Listed Journal
Association with Indian Institute of Public Administration
Current Volume: 16 (2024 )
ISSN: 2249-2577
Periodicity: Quarterly
Month(s) of Publication: मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर
Subject: Social Science
DOI: https://doi.org/10.32381/LP
लोक प्रशासन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की एक सहकर्मी समीक्षा वाली त्रैमासिक शोध पत्रिका है ! यह UGC CARE LIST (Group -1 ) में दर्ज है ! इसके अंतर्गत लोक प्रशासन, सामाजिक विज्ञान, सार्वजनिक निति, शासन, नेतृत्व, पर्यावरण आदि से संबंधित लेख प्रकाशित किये जाते है !
EBSCO
अध्यक्ष एवं सम्पादक महानिदेशक, आई. आई. पी. ए. सह-आचार्या, संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानून, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश क्षेत्रीय शाखा (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) आचार्य, हाजीपुर, बिहार आचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली भा. प्र.से., प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ओडिशा सरकार सह-आचार्य, विकास अध्ययन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली कुलसचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
श्री एस. एन. त्रिपाठी
नई दिल्ली
सह-सम्पादक
सपना चड्डा
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
सम्पादक मंडल
के.के. सेठी
डा0 शशि भूषण कुमार
प्रो. श्रीप्रकाश सिंह
शुभा सर्मा
डा0 साकेत बिहारी
श्री अमिताभ रंजन
पाठ सम्पादक
स्नेहलता
Volume 16 Issue 4 , (Oct-2024 to Dec-2024)
शिक्षा पर नवीन शिक्षण दृष्टिकोणों के प्रभाव का आकलनः एक समीक्षा
By: जगदीप सिंह , अक्षय राज शर्मा
Page No : 1-13
Abstract
दुनिया भर में कई शैक्षिक प्रणालियों में नवीन शिक्षण दृष्टिकोणों का उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो गया है। यह समीक्षा पत्र शिक्षा पर नवीन शिक्षण दृष्टिकोणों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। विश्लेषण मौजूदा साहित्य की समीक्षा पर आधारित है, जो छात्रों के सीखने के परिणामों और शैक्षणिक उपलब्धि पर नवीन शिक्षण प्रथाओं के प्रभाव पर केंद्रित है। यह शोध पत्र समस्या-आधारित शिक्षा, मिश्रित शिक्षा, गेमीफिकेशन और फ़्लिप सीखने जैसी विभिन्न पद्धतियों की जाँच करता है। यह अध्ययन, छात्र प्रेरणा, जुड़ाव और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाने में नवीन शिक्षण दृष्टिकोणों के सकारात्मक प्रभावों की पहचान करता है। यह नवीन शिक्षण दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से लागू करने में शिक्षक प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। निष्कर्ष बताते हैं कि अभिनव शिक्षण विधियों में स्कूलों में शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है। हालांकि, छात्र परिणामों में सुधार के लिए इन दृष्टिकोणों के दीर्घकालिक प्रभाव और स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए और शोध की आवश्यकता है।
Authors
डॉ. जगदीप सिंह, सहायक प्राध्यापक - व्यावसायिक प्रबंधन अध्ययन विभाग, क्रिस्तु जयंती कॉलेज, बेंगलुरु, कर्नाटक।
अक्षय राज शर्मा, पीएचडी स्कॉलर, कंप्यूटर विज्ञान और आईटी विभाग, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.1
Price: 251
भारतीय संविधान के पचहत्तर वर्ष: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
By: संतोष कुमार सिंह
Page No : 14-31
Abstract
किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। अतएव भारतीय संविधान के आधुनिक और विकसित स्वरूप को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान अनिवार्य है। भारतीय संविधान, अपने निर्माताओं की दूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण है। इसने शासन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की जटिलताओं तथा चुनौतियों के बीच राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। सटीकता और लगन के साथ तैयार किए गए इस आधारभूत दस्तावेज ने भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विरासत के विविधता से परिपूर्ण ताने-बाने को एक साथ बुना है। भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की आधारशिला को सशक्त किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के जिस संविधान का निर्माण किया है, उसमें भारत की प्राचीन संस्कृति के सिद्धान्तों और मूल्यों के प्रत्येक आयाम को स्पर्श किया है। अतः भारत का संविधान हर कालखंड में जनहित की कसौटी पर खरा उतरने के साथ-साथ अपनी निरंतरता, उपयोगिता और प्रासंगिकता को सदैव सिद्ध किया है। भारत अपने संविधान के 75 वर्ष ( 26 नवम्बर, 1949 - 26 नवम्बर, 2024) पूर्ण होने पर पर्व मना रहा है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान की गरिमापूर्ण यात्रा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।
Author
संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला - खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.2
Price: 251
महिलाएँ, पंचायत और आरक्षणः एक विश्लेषण
By: रिंकी
Page No : 32-38
Abstract
वर्तमान संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में 73वें संविधान संशोधन की भूमिका के महत्त्व को स्वीकार किया जाता रहा है। जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर महिलाओं की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। समय-समय पर पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते रहें हैं। इस संदर्भ में इस पेपर के अंतर्गत यह देखने का प्रयास किया गया है कि इतने वर्षों के पश्चात भी क्या वास्तव में इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित् हो पाई है या महिलाएँ अभी भी इस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक व पितृसत्ता के प्रभावों को झेलती हैं। वर्तमान समय में इस तथ्य को मेरे द्वारा हरियाणा राज्य में मनरेगा जैसी नीतियों के संदर्भ में प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से परखा गया है जहाँ मनरेगा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गयी है। जिसमें महिलाएँ नीतियों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन व महिलाओं के कल्याण में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। मनरेगा में महिला सरपंचों की भूमिका महिलाओं के कल्याण में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस परिस्थिति में परिवर्तन न सिर्फ महिलाओं के कल्याण के लिए आवश्यक है बल्कि नीतियों की सफलता के लिए भी आवश्यक है।
Author
रिंकी, सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.3
Price: 251
लैंगिक न्याय एंव पुलिस प्रशासन
By: शिवानी सिंह
Page No : 39-54
Abstract
"नार्यस्तु राष्ट्रस्य स्वः," स्त्री राष्ट्र का भविष्य होती है। एक राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अतुलनीय है। भारतीय संविधान ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का अधिकार प्रदान किया है। समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। पुलिस बल में महिलाओं की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की है। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस बल में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आये हैं किंतु ये परिवर्तन पर्याप्त नहीं हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और इस युग की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अब वह रूढ़ीवादी परम्पराओं, सामाजिक कुरीतियों और पितृसत्तात्मक का खुलकर विरोध कर रहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में भी उनकी स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। प्राचीन समय में पुलिस बल में महिलाओं को इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाता था क्योंकि उन्हें कमजोर, कोमल और इस पेशे के लिए शारीरिक रूप से अनुपयुक्त माना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् भी उच्च पदों (आई.पी.एस) पर प्रवेश के लिए दशकों लग गए। तत्पश्चात् 1973 में किरण बेदी ने अपने अथक प्रयास और संघर्ष के बाद उच्च पदों पर महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। विशेष रूप से पुलिस विभाग में महिलाओं की स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। 2022 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल दो लाख 15 हजार 504 महिला पुलिस कर्मचारी है जो संपूर्ण पुलिस बल का मात्र 10.03 प्रतिशत ही है।
Author
शिवानी सिंह, शोध छात्रा, लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.4
Price: 251
By: विनोद कुमार त्रिवेदी
Page No : 55-75
Abstract
किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा तथा उसकी विकास और आर्थिक प्रगति के बीच एक घनिष्ठ संबंध मौजूद रहता है। समृद्धि और आर्थिक विस्तार के लिए एक स्थिर और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र आवश्यक है क्योंकि कोई भी देश अस्थिर वातावरण में विकास और उन्नति नहीं कर सकता। यदि हम भारत के सुरक्षा तंत्र की बात करें तो पाएंगे कि यहाँ एक बहुत ही जटिल आंतरिक सुरक्षा संरचना अस्तित्व में है, जिसमें कई एजेंसियां समान तरह के कार्य कर रही हैं और साथ ही, यह आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना भी कर रही है। जिसमें मुख्यतः देश के समक्ष मौजूद सुरक्षा चुनौतियों जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और अंतर-सांप्रदायिक संघर्ष जैसे पारंपरिक खतरों से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण की प्रगति द्वारा लाई गई नए युग की चुनौतियाँ जैसे साइबर सुरक्षा, डिजिटल युद्ध, डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चुनौतियाँं, सोशल मीडिया पर गलत सूचना से लेकर प्रौद्योगिकी-आधारित जासूसी तक सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण और जलवायु संबंधी चुनौतियाँ, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और महामारी, जैविक और परमाणु खतरे, संसाधन आवंटन तथा जातीय और भाषाई संघर्ष जैसी समकालीन उभरती जटिलताएं कुछ ऐसी हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए समान रूप से खतरनाक हैं। ये चुनौतियाँं गतिशील प्रकृति की हैं जिनसे निपटने हेतु समय रहते रणनीतिक सोच और अनुकूलनीय नीतियों के साथ राष्ट्र की व्यापक आंतरिक सुरक्षा संरचना पर काम करने की जरूरत हैं। इस हेतु देश के उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों के पुनर्गठन और पुनः आवंटन के माध्यम से देश का एक कॉम्पैक्ट, एकीकृत और भविष्योन्मुख आंतरिक सुरक्षा ढाँचा तैयार किया जाए जिससे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जा सके एवं देश में उपलब्ध सुरक्षा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सके। यह आंतरिक सुरक्षा सुधारों और अन्य प्रमुख देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) को अपनाते हुए मौजूदा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। 2047 के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत आंतरिक सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए समान तरह से कार्य कर पाने में सक्षम संस्थानों एवं बलों के एकीकरण एवं पुनर्गठन के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मितव्ययी और चुस्त बनाने की आवश्यकता हैं।
Author
विनोद कुमार त्रिवेदी, रिसर्च स्कॉलर और ग्रुप ए अधिकारी सीआरपीएफ कैडर (2005 बैच) वर्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत हैं।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.5
Price: 251
भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा एवं दशाः हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में एक समीक्षा
By: राजबीर सिंह दलाल , संदीप ढिल्लों
Page No : 76-91
Abstract
प्रस्तुत शोध पत्र महिला सशक्तिकरण के बहुआयामी मुद्दे पर गहन चर्चा करता है और लोकतांत्रिक युग में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। लोकतांत्रिक प्रगति महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की सक्रिय भागीदारी से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं की भूमिका में उतार-चढ़ाव रहा है। प्राचीन काल में सापेक्ष समानता की पेशकश की गई थी, जो विभिन्न सामाजिक-धार्मिक मानदंडों के कारण समय के साथ खराब होती गई। प्रस्तुत शोध विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश पर केंद्रित है। आर्थिक प्रगति के बावजूद राज्य में लिंग असमानताओं को देखा सकता हैं। भारत में सबसे कम महिला लिंग अनुपात, उच्च मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के सामने आने वाली व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को प्रदेश में देखा जा सकता हैं। निष्कर्ष महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में धीमे लेकिन सकारात्मक बदलाव, महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि और दमनकारी परंपराओं में धीरे-धीरे कमी दर्शाते हैं। हालाँकि, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहसों और राजनीतिक संगठनों में उनकी भागीदारी में महत्वपूर्ण अंतर अभी भी बना हुआ है। अध्ययन में हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रणनीतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों की माँग की गई है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
Authors
राजबीर सिहं दलाल, विभागाध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा।
संदीप ढिल्लों, सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद, हरियाणा।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.6
Price: 251
भारतीय प्रशासनिक परिदृश्य पर वैश्वीकरण का प्रभाव
By: स्वाति सुचारिता नंदा , राकेश कुमार मीना
Page No : 92-107
Abstract
यह शोधपत्र लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर केंद्रित है। भारतीय समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना आम बात है। हालाँकि, भारतीय प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभावों को अभी भी ठीक से प्रलेखित नहीं किया गया है, भले ही इसके प्रभाव संरचना और कार्यों दोनों के संदर्भ में दूरगामी रहे हों। संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच, वैश्वीकरण ने नई इकाइयाँ शुरू की हैं जो भारतीय प्रशासन को इसके पारंपरिक हस्तक्षेपवादी संगठन से नियामक प्रकृति की ओर ले जाती हैं। कार्यात्मक रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी के युग ने कई ऐसे कार्य लाए हैं, जो लाभ को उद्देश्य के रूप में शामिल करने की दिशा में कल्याणकारी ढाँचे से बहुत आगे निकल गए हैं। इसने प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र में और भी गहरे बदलाव किए हैं क्योंकि ‘प्रशासक-नागरिक’ संबंध ‘प्रबंधक-ग्राहक’ संबंध में बदल गया है। वर्तमान शोधपत्र प्रशासनिक परिदृश्य में उन परिवर्तनों पर चर्चा करने पर केंद्रित है जो भारत द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद से हुए हैं।
Authors
स्वाति सुचारिता नंदा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, डीएवी पीजी कॉलेज, वाराणसी।
राकेश कुमार मीना, सहायक प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह कॉलेज, नई दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.7
Price: 251
By: प्रीति चाहल
Page No : 108-116
Abstract
गाँधीजी ने सत्य को ईश्वर के समकक्ष रखा है और उसे प्राप्त करने का साधन अहिंसा बताया इस अहिंसा के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही रूपों की उन्होंने व्याख्या की है। नकारात्मक रूप में तो यह किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाना है। तो सकारात्मक रूप में यह मनुष्य को क्या करना चाहिए का निर्देश देता है। अर्थात् यह ’मानव प्रेम’ को बढ़ावा देता है। बाइबिल के वाक्यों को दोहराते प्रेम को बढ़ावा देता है। बाइबिल के वाक्यों को दोहराते हुए गाँधी कहते हैं “पाप से घृणा करे, पापी से नहीं।“ अर्थात् अपने चरित्र बल द्वारा वे विरोधियों या अन्यायियों के ’हृदय परिवर्तन’ पर बल देते हैं। अहिंसा को और भी व्यापक रूप से समझाते हुए उन्होंने कहा है कि, किसी को कष्ट पहुँचाने का विचार या किसी का बुरा चाहना भी हिंसा है। किसी के प्रति घृणा या द्वेष का भाव रखना भी हिंसा है। आवश्यकता से अधिक वस्तु ग्रहण करना तथा पर्यावरण में किसी तरह का गन्दगी या प्रदूषण फैलाना भी अहिंसा है“।
गाँधी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अहिंसा निर्बल व्यक्ति का आश्रय नहीं, वरन् शक्तिशाली का अस्त्र है। विरोध के शान्ति से डर जाना या अत्याचार के विरूद्ध बल प्रयोग न कर पाना अहिंसा नहीं वरन् यह नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति या समूह का बल है जो सत्य पर दृढ़ निष्ठा से प्राप्त होता है। इसका सबसे अच्छा साधन ’सत्याग्रह’ है गाँधीजी ने कहा कि सत्याग्रही कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। सत्य की सिद्धि कठिन तो है, परन्तु अनन्तः सत्य की ही विजय होती है - ’सत्यमेव जयते नामृताम’। इसके साथ ही गाँधीजी ने अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह को मिलाकर ’सविनय अवज्ञा’ आंदोलन की संकल्पना को भी प्रतिपादित किया था।
ईश्वर अथवा एक सर्वव्यापी आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास गाँधी का मूल तत्व है। अपने जीव में वे टाल्सटाँय, रस्किन, थोरी, स्वामी विवेकानन्द, गोखले जैसे व्यक्तियों से अपने जीवन में प्रभावित थे। उनका कहना था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है। गाँधीजी के अनुसार आत्मानुभूति का अभिप्राय ईश्वर को आमने सामने देखना है, अर्थात् चरम सत्य महसूस करना है, जिसे अपने आप को भी मानना कहा जा सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि इसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक मनुष्य सम्पूर्ण मनुष्य जाति में स्वयं को न ला सके। इसमें अनिवार्यतः राजनीति भी सम्मिलित है।
Author
प्रीति चाहल, एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.8
Price: 251
उत्तराखंड राजनीति एवं महिला उत्थान - एक विश्लेषण
By: अनामिका चौहान
Page No : 117-132
Abstract
उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान की प्रक्रिया समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर सामने आई है। राज्य की महिलाएँ अपनी पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए विभिन्न आंदोलनों और संगठनों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। चिपको आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने जंगलों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने न केवल पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के नए आयाम दिए। इसके अलावा, पंचायत चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण, उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुए हैं। उत्तराखंड में महिलाओं को अब भी कई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पितृसत्तात्मक समाज, शिक्षा की कमी, और आर्थिक निर्भरता। फिर भी, महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और स्वरोजगार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न अभियान, जैसे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ“ और “महिला सुरक्षा अभियान“, ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। इस लेख में उत्तराखंड में महिला उत्थान की प्रक्रिया और इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।
Author
अनामिका चौहान, सहायक प्रोफेसर, चमनलाल महाविद्यालय, लंढौरा, हरिद्वार, उत्तराखंड।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.9
Price: 251
मतदान व्यवहार और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन- सैद्धांतिक विश्लेषण
By: राकेश कुमार , विकास तिवारी
Page No : 133-146
Abstract
चुनाव लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए नागरिकों का मतदान व्यवहार अधिक महत्व रखता है। क्योंकि यह व्यवहार ही प्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ता मिलने या खोने का निर्धारण करता है। इसलिए मतदान व्यवहार को सभी राजनीतिक अभ्यासों का केंद्र बिंदु माना जाता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन अब अध्ययन के क्षेत्र में स्वतंत्र विषय के रूप में देखा जाता है। सामाजिक दबावों, आर्थिक लाभ, मनोवैज्ञानिक सुझावों और सबसे बढ़कर, चुनाव अभियान के प्रभाव ने मतदान के निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक व्यापक रूप से जटिल गतिविधि बना दिया है। मतदान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक मतदान व्यवहार का निर्माण करते है जिसे अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उदेश्य उन दृष्टिकोणों को समझना है जिसके तहत मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है। इस अध्ययन में मतदान व्यवहार के सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है।
Authors
राकेश कुमार, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
विकास तिवारी, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.04.10
Price: 251
Jan- to Mar-2024
By: ..
Page No : i-v
भारत में एफडीआई के लिए नीतिगत पहलः मेक इन इंडिया के विशेष सन्दर्भ में
By: सोनम
Page No : 1-17
Abstract
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक है, जो देश के विकासात्मक प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण गैर-ऋण वित्तीय भंडार बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय निगम रणनीतिक रूप से भारत में निवेश करते हैं, कर प्रोत्साहन और अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी श्रम लागत सहित देश के अद्वितीय निवेश प्रोत्साहनों का लाभ उठाते हैं। यह तकनीकी विशेषज्ञता के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है और रोजगार सृजन और विभिन्न सहायक लाभों को बढ़ावा देता है। भारत में इन निवेशों का आगमन सीधे तौर पर सरकार की सक्रिय नीति ढांचे, एक गतिशील कारोबारी माहौल, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और बढ़ते आर्थिक प्रभाव का परिणाम है।
यह लेख भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई के महत्व पर चर्चा करता है, यह एफडीआई को आकर्षित करने के लिए उठाए गए हालिया उपायों पर भी प्रकाश डालता है, मुख्य रूप से मेक इन इंडिया अभियान पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अभियान की सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाओं पर भी चर्चा की गई है।
Author :
डाॅ. सोनम : वाणिज्य विभाग, शहीद भगत सिंह, सांध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.1
Price: 251
भारत के चुनाव आयोग की बदलती भूमिकाः मुद्दे और चुनौतियां
By: अनिल कुमार
Page No : 18-33
Abstract
भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय भारत निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते, संसद और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव कराना भारत के चुनाव आयोग के लिए सहज काम नहीं है। हर चुनाव में एक खामी रह जाती है जो भारत के चुनाव आयोग को कुशल बनने और जनता की नजरों में एक बेदाग छवि बनाने में बाधा डालती है। चुनावों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे बुनियादी ढांचे, वित्त, कर्मियों, नागरिकों और मतदाताओं के बीच जागरूकता की कमी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ समन्वय, राजनीतिक दबाव, नामांकन दाखिल करना, धन और बाहुबल का दुरुपयोग, खर्च की सीमा, फंडिंग पैटर्न से संबंधित कई मुद्दे, राजनीति के अपराधीकरण की जाँच, चुनावी धोखाधड़ी, स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची का दोहराव और भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण आदि। भारत के चुनाव आयोग की पारंपरिक भूमिका और कार्य समय की आवश्यकता और प्रगति के अनुसार बदलते रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावों में कदाचार की जाँच के लिए विभिन्न तरीकों से आवश्यक कदम उठाए हैं। यह पत्र आयोग की वास्तविक स्थितियों और समस्याओं को जानने का प्रयास करता है और भारत के चुनाव आयोग के सामने आने वाले मुद्दों, समस्याओं और चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन करता है। अध्ययन भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट और कुछ प्रकाशित लेखों के माध्यम से किया गया है।
Author :
डाॅ अनिल कुमार : सहायक आचार्य लोकप्रसासन विभाग, सी. डी. ओ. ई. एजुकेशन, पंजाब विश्वविधालय, चंडीगढ़।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.2
Price: 251
भारतीय न्यायपालिका पर मीडिया ट्रायल का प्रभावः आलोचनात्मक विश्लेषण
By: आशुतोष मीणा
Page No : 34-44
Abstract
निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका की कार्यवाही में विधायिका व कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के आधार पर मीडिया समाचारों की रिपोर्टिंग करता है। मीडिया द्वारा अदालतों में विचाराधीन मामलों की सनसनीखेज रिर्पोटिंग कर दी जाती है जिससे न्यायपालिका के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने व न्यायिक निर्णय प्रभावित होने की संभावना रहती है। हाई प्रोफाइल मामलों में मीडिया द्वारा अनवरत रिपोर्टिंग से मामले को इतना प्रचारित कर दिया जाता है कि न्यायधीश कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों व सबूतों से इतर अलग धारणा बना सकते हैं। मीडिया द्वारा बनाए गए माहौल से न्यायधीश की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। मीडिया ट्रायल न्यायधीश को आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर सकती है, भले ही आरोपी निर्दोष हो। यह शोध पत्र इस बात पर केंद्रित है कि मीडिया ट्रायल आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। शोध पत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के बीच टकराव पर प्रकाश डाला गया है।
Author :
डाॅ. आशुतोष मीणा : एसोसिएट प्रोफेसर, लोकप्रशासन, राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतान (दौसा)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.3
Price: 251
वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था
By: लुके कुमारी
Page No : 45-61
Abstract
भारतीय न्यायिक व्यवस्था मूल रूप से अंग्रेजी न्यायिक संहिता पर आधारित है। जिसे हम भारतीय आपराधिक दंड संहिता तथा भारतीय नागरिक संहिता के मध्य विभाजित कर सकते हैं आपराधिक दंड संहिता के दो हिस्से हैं। प्रथम, तात्विक न्याय तथा प्रक्रियात्मक न्याय। इन्हीं के मध्यनजर भारत में विवादों के समाधान की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। हम जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में न्यायाधीशों और न्यायालयों की कम संख्या न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को बाधित करती है। न्याय की मूल माँग है कि उचित समय में व्यक्ती को उसका हक प्राप्त हो सके। वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली को वह आधार प्रदान करती है जिससे कि न्याय की पहुँच पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति को भी प्राप्त हो सके।
Author :
लुके कुमारी : सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, भारती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.4
Price: 251
भारत में जल अभिशासनः सैद्धांतिक और क़ानूनी पृष्ठभूमि
By: विकास कुमार
Page No : 62-74
Abstract
इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ तक यह स्पष्ट हो गया कि दुनिया जल संकट की अवस्था से गुजर रहा है जिसका असर आम-आदमी सहित सरकारों के काम-काज पर भी समान रूप से दिखाई देने लगा है। लेकिन इस समस्या की प्रमाणिकता को लेकर आम चर्चा और बहस 1970 के दशक के बाद से प्रारंभ हुई। इस बहस ने इस बात को स्थापित किया कि दुनिया की एक बड़ी आबादी के पास स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है जो एक तरह से आम जनमानस और सरकारों के लिये संकट का उद्घोष है। देश-दुनिया में इसके कारणों को लेकर छिड़ी बहस से मुख्यतौर पर दो तरह के विश्लेषण उभर कर सामने आए। पहला, ‘माल्थुसियन प्रभाव’, जो संसाधनों की कमी, जनसंख्या का दबाव और सीमित विकास के संदर्भ में था। लेकिन दो दशक बाद ही जल संकट को लेकर दूसरा विश्लेषण मुख्य धारा में स्थापित हो गया जिसका मानना था कि विश्व में जल संकट की समस्या से जूझ रहे अधिकांश क्षेत्र राजनीति, गरीबी और पानी के प्रबंधन और उसके असमान आवंटन का परिणाम हैं। संक्षेप में, यह माना गया की मूल रूप से जल संकट दोषपूर्ण ‘अभिशासन’ का परिणाम है। इसकी पुष्टि सन् 2000 में प्रकाशित 'वल्र्ड वाटर काउंसिल’ की रिपोर्ट विस्तृत रूप से करती है जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ‘जल संकट’ उसके प्रबंधन पद्धति का परिणाम हैं और इससे वर्तमान समय में दुनिया के अरबों लोग और पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रस्तुत पत्र भारत में जल अभिशासन से सबंधित बनाए गए कानूनों और उसके सैद्धांतिक विमर्श पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के स्वरूप और उसके प्रभावों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है।
Author :
विकास कुमार : राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.5
Price: 251
जनसांख्यिकीय लाभांशः आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देश
By: मयंक भारद्वाज , आशीष रंजन , ज्योति शर्मा
Page No : 75-88
Abstract
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (12 मई, 2020) ने ‘‘आत्मनिर्भर भारत‘‘ के लिए आह्वान किया, जिसमें इसके पांच स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में जीवंत जनसांख्यिकी के महत्व पर जोर दिया गया। भारत वर्तमान में एक युवा आबादी से संपन्न देश है, जिसके नागरिक नवीन विचारों और उद्यमशीलता की भावना से ओत-प्रोत है। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए आश्वस्त है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में, 65 प्रतिशत से अधिक आबादी की आयु 35 वर्ष से कम है, और आधे से अधिक आबादी 15-59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में आते हैं। यह जनसांख्यिकीय लाभ एक बहुमूल्य कार्यबल प्रदान करता है जो भारत के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि, इन लाभों को अधिकतम करने हेतु, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए कुशल संरचनाओं और तंत्रों को स्थापित करना आवश्यक है। भारत ने अमृतकाल में कदम रखा है, जो हमारे युवाओं के लिए अपनी क्षमताओं का लाभ उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्रगति के रास्ते में युवाओं के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। अवसरों के साथ रचनात्मकता आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को तेज करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगी।
Authors :
श्री मयंक शर्मा : शोध छात्र, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
प्रो. आशीष रंजन : आचार्य, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
प्रो. ज्योति शर्मा : आचार्य, कलस्टर इनोवेशन सेन्टर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.6
Price: 251
भारत में शिक्षा क्षेत्र में नीतियों और उपलब्धियों का आकलन
By: प्रवीण कुमार झा , विनायक राय , संगीता
Page No : 89-101
Abstract
आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि “हमारी आबादी के बड़े हिस्से को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं कैसे प्रदान की जाएं जो वर्तमान में इन सेवाओं से वंचित हैं।” शिक्षा वह महत्वपूर्ण कारक है जो गरीबों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने की क्षमता रखती है। यह स्पष्ट है क्योंकि शिक्षा ही विकास-सुधार का मूल निर्धारक कारक है। यह, एक ओर, मानव क्षमता को विकसित करने में मदद करता है, दूसरी ओर सक्षम लोगों को विकसित करने में मदद करता है। आज नागरिकों को राष्ट्र के विकास के कार्य में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सरकार इन मापदंडों के तहत स्थितियों को ऊपर उठाने के लिए नई और अभिनव योजनाएं बना रही है और संसाधनों का आवंटन कर रही है लेकिन क्या वह लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है? आज क्या हम वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को विकसित कह सकते हैं? देश में कुछ हद तक आर्थिक और सामाजिक प्रगति तो हुई है लेकिन क्षेत्रवार, जातिगत और लिंगवार में समान रूप से प्रगति नहीं हुई है। इस लेख का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई नीतियों और उनके कार्यान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है ताकि इसकी सीमित सफलता के कारण और भविष्य में हमारे बेहतर स्थिति (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासात्मक पैमाने पर) के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले विकल्पों का पता लगाया जा सके।
Authors :
प्रो. (डाॅ.) प्रवीण कुमार झा : प्रोफेसर, राजनीतिक विभाग, शहीद भगत सिंह काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
श्री विनायक राय : एम काॅम, दिल्ली विश्वविद्यालय।
प्रो. (डाॅ.) संगीता, प्रोफेसर : राजनीतिक विभाग, शहीद भगत सिंह काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.7
Price: 251
डॉ. अम्बेडकर की समावेशी समाज की संकल्पना: एक विश्लेषण
By: विजय शंकर चौधरी , देवेंद्र मौर्य
Page No : 102-114
Abstract
भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को लेकर एक समावेशी दृष्टिकोण था, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को इसके अंतर्गत शामिल करने एवं सशक्त करने पर जोर देता है। उनका मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र आदर्श समाज के दो अनिवार्य घटक हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनका दृढ़ मत था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगी। डॉ. अम्बेडकर एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली में विश्वास करते थे जहाँ प्रत्येक नागरिक के पास अपने देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और योगदान करने के समान अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के महत्व पर जोर दिया, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी जाति, नस्ल, लिंग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वतंत्र मतदान करने का अधिकार हो। समाज के वंचित तबको को निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की वकालत की। डॉ. अम्बेडकर एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के समर्थक थे जो संपत्तियों और संसाधनों के समान वितरण की व्यवस्था समाज के सभी वर्गों के लिए सुनिश्चित करती है। उनका मानना था कि संसाधनों और उत्पादन के साधनों तक पहुँच सामाजिक या आर्थिक स्थिति के बजाय योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने पूँजीपतियों के विकल्प के रूप में सहकारी समितियों के गठन की भी वकालत की, जिससे कामगारों को उत्पादन उपकरण और मशीनरी प्राप्त करने में सुगमता हो सके और साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में वे अपनी बात रख सके । अगर हम वर्तमान में देखे तो डॉ बी. आर. अम्बेडकर जिस राजनीतिक लोकतन्त्र की बात कर रहे थे उसे हमारे सविंधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर उसको प्राप्त करने की कोशिश की गई है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की र्गइ है । अगर आर्थिक समानता की देखें तो जिस तरह से देश में सम्पतियों का असमान वितरण हो रहा है और चुनावी प्रक्रिया में पूंजी का दखल बढ़ रहा है, वह कहीं न कहीं अम्बेडकर के राजनीतिक और आर्थिक समता पर आधारित लोकतांत्रिक एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर रही है ।
प्रस्तुत आलेख डॉ. अम्बेडकर के राजनैतिक और आर्थिक समावेशी समाज के परिप्रेक्ष्य और संदर्भो पर आधारित चिंतन को व्याख्यायित करता है ।
Authors :
विजय शंकर चौधरी : शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)।
देवेंद्र मौर्य : शोधार्थी, गाँधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.8
Price: 251
राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से समावेशी सामाज का दर्शन
By: शिव कुमार मीणा
Page No : 115-126
Abstract
राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण पर्यटन अपेक्षाकृत एक नया पक्ष है। राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन समावेशी समाज का महत्वपूर्ण औजार बना है। ‘‘राज्य में विभिन्न जातीय संघटन व सांस्कृतिक स्वरूपों के समूह है। यहाँ भील, मीणा, डामोर, गरासिया जनजातियाँ विद्यमान है।’’ (भार्गव, 2011, 101) यह जनजातियाँ मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही व बरन जिलों में स्थापित है। इन जनजातियों का विकास करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक व दैनिक जीवनचर्या से बिल्कुल कटे हुए है। ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से इनके सामाजिक व आर्थिक स्तर को उठाया जा सकता है। यह जनजातीय लोग ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संपर्क में आएंगे, जिससे उनके सोचने समझने के दायरे में विस्तार होगा। आज विश्व के लोग इन जनजातियों के भोजन, सांस्कृतिक, वेशभूषा, हस्तशिल्प, त्यौहार आदि के प्रति आकर्षित हो रहे है। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जनजातीय लोगों का विकास होता है। इन जनजातियों के बीच ग्रामीण पर्यटन को लेकर रूचि बढे़ और वह इसमें भाग लें। इसके लिए सरकार व स्वयं सेवी संगठनों को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि जनजातीय लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिलें। इस शोध में ग्रामीण पर्यटन द्वारा राजस्थान के ग्रामीण समावेश पर चर्चा की गई है। यह अध्ययन पुस्तकों, जर्नल, रिपोर्ट व जनगणना 2011 आदि से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।
Author:
शिव कुमार मीणा : पी.एच.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.9
Price: 251
सहकारिता और शिक्षा का समन्वयः युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में
By: मल्लिका कुमार
Page No : 127-143
Abstract
इस शोध पत्रिका में शिक्षा के संदर्भ में सहकारिता के मूल्यांकन को प्रस्तुत किया है। इसमें वर्तमान में बेरोजगारी एवं असमानता की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि किस तरह ये सहकारी समितियाँ एक जन-केंद्रित ढाँचे (मॉडल) के रूप में उन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती हैं। सहकारिता का अर्थव्यवस्था के विकास में विशेष योगदान है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने दूसरी बार वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता से समृद्धि के लिए, भारत में जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। अब पाठ्îक्रम में भी सहकारी शिक्षा को एकीकृत करने और युवाओं को सहकारिता के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया गया है। और यह विश्वास जताया है कि शिक्षकों, संस्थानों, युवाओं और समुदायों के सहयोग से सहकारिता द्वारा देश का समावेशी और सतत् विकास होगा।
Author :
डॉ. मल्लिका कुमार : उपाध्यक्ष, शिक्षण संस्थानों में सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (ICA-AP) समिति, सह-प्राध्यापिका, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.01.10
Price: 251
Apr- to Jun-2024
By: प्रो. अशोक विशनदास
Page No : v-vii
भारत में ‘एक देश एक चुनाव’: संभावना और चुनौतियां
By: विनीत कुमार सिन्हा
Page No : 1-15
Abstract
‘‘एक राष्ट्र एक चुनाव‘‘ भारत में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव चक्रों को समकालिक करने का एक प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ चुनाव कराना है। समर्थकों का तर्क है कि यह चुनाव खर्च को कम कर सकता है, स्थिर शासन प्रदान कर सकता है, मतदायित्व प्रतिशत बढ़ा सकता है और प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर सकता है। आलोचक संवैधानिक चुनौतियों, तार्किक जटिलताओं, क्षेत्रीय मुद्दों के संभावित प्रभाव और राजनीतिक सर्वसम्मति की आवश्यकता के बारे में चिंता जताते हैं। यह लेख देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर चर्चा करता है और साथ ही भारत में एक साथ चुनाव कराने में संभावित बाधाओं का पता लगाने का प्रयास करता है और इसके लिए एक रोडमैप दर्शाने का भी एक प्रयास करता है।
Author: डॉ. विनीत कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.1
Price: 251
सामाजिक योजनाओं के परिशोधन में नागरिक फीडबैक: सुशासन की आवश्यकता
By: युवराज कुमार
Page No : 16-26
Abstract
जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कल्याणकारी राज्य है। जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अध्याय चार अनुच्छेद 36 से 51 ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों’ के अंतर्गत किया गया है। वास्तव में ‘निदेशक सिद्धांत’ प्रत्येक शासन एवं प्रशासन की सफलता और असफलता का एक प्रमाणपत्र है। इसमें समाज में रहने वाले सभी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग से संबंधित, सरकार को लोक कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों तथा कानूनों का निर्माण के लिए निर्देश दिए गए है। निर्देशक सिद्धांत के अनुरूप ही कल्याणकारी योजनाएं बनायीं जाती हैं। बजट के दौरान इन योजनाओं की घोषणा तथा समय-समय पर नीति एवं कानूनों का निर्माण करके इनका क्रियान्वयन किया जाता है। इन योजनाओं और कानूनों का प्रभाव एवं परिणाम दोनों नागरिकों के प्रभाव एवं लाभ पर निर्भर करता है। इसी आधार पर नागरिक, सरकार के कार्य, नीतियों एवं योजनाओं तथा कानूनों का समर्थन करते हैं। परिणामस्वरूप आने वाले चुनावों में जनता सरकार को पुनः समर्थन देकर या निर्वाचित करके सत्ता में आसीन रखती है या सिरे से नकार देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह कल्याणकारी योजनाएं वास्तव में नागरिकों के फीडबैक (प्रतिक्रिया) के द्वारा सरकारों की सफलता और असफलता का एक मापदंड है।
Author : डाॅ. युवराज कुमार, सहायक आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.2
Price: 251
डजिटल लामबंदीकरण और पर्यावरणीय जागरूकताः एक विश्लेषण
By: मनीष कुमार , सुजीत कुमार चौधरी
Page No : 27-39
Abstract
आज विश्व के समक्ष पर्यावरणीय समस्याएँ सभी समस्याओं में सर्वोपरि हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित दोहन और पर्यावरणीय नैतिकता का तथाकथित विकसित होनें के क्रम में पीछे छूटना एक अंधकारमय भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। समस्त राष्ट्रों और उनकें लोगों के बीच आभासीय मंचन के द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और परिस्थितिकीय समस्याओं को लेकर गंभीर संवाद की उपस्थिति दर्ज होती दिख रही है (बेनेट एवं अन्य, 2014)। यह अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सोशल मीडिया के द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता को प्रखर बनानें की भूमिका की पड़ताल करता है। विगत कुछ वर्षो में पर्यावरण के संतुलन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं। आज इन समस्याओं का समाधान आभासी पटल पर खोजा जा रहा है। आज सभी समस्यात्मक विषय डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। समस्याओं के निराकरण हेतु डिजिटल लामबंदीकरण की जा रही है, जिसकी पहुँच महानगर से लेकर गाँव तक सुलभ हो रही है। यह शोध पत्र मुख्य रूप से पर्यावरणीय नैतिकता और जागरूकता में डिजिटल पटल की भूमिका और डिजिटल लामबंदीकरण की प्रकिया पर प्रकाश डालता है।
Authors:
श्री मनीष कुमार : पीएच.डी स्कॉलर, समाजशास्त्र-विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
डा. सुजीत कुमार चौधरी : सह आचार्य और विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र-विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.3
Price: 251
भारतीय ज्ञान परंपराः शिल्प शास्त्र का सामाजिक पहलू
By: नीना बंसल
Page No : 40-57
Abstract
भारतीय संस्कृति में ‘ज्ञान’, ’कला’ और ‘कौशल’ पर व्यापक ध्यान दिया गया, जो शिक्षा के समग्र एवं विविध दृष्टिकोण का सूचक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ‘शिल्प’ भी कला का प्रतीक है, जबकि ‘शास्त्र’ विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ’शिल्प शास्त्र’ सामूहिक रूप से कला और शिल्प के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के कई मंदिरों और मूर्तियों में आज भी इस तरह की शैली स्पष्ट रूप से विद्यमान है। मंदिर की वास्तुकला सदियों में विकसित हुई है, तथा बदलते राजवंशों और क्षेत्रों के साथ-साथ शैली भी बदली। आम आदमी के लिए मंदिर को पूजा स्थल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परन्तु दार्शनिक स्तर पर यह और भी बहुत कुछ दर्शाता है। प्रस्तुत लेख के द्वारा भारतीय सभ्यता में पल्लवित और पुष्पित प्राचीन ज्ञान के क्षेत्रों की महत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास है, जिससे हम अपनी सभ्यता और उसकी प्राचीन विरासत को समझने और समझाने के लिए ज्ञान की इस शक्तिशाली कुंजी का प्रयोग सहज होकर कर सकें। इस शोधपत्र का मूल उद्देश्य यह है कि किसी भी सभ्यता का प्राचीन ज्ञान जैसे शिल्प, वास्तु, कला, संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य, आध्यात्मिकता व अन्य संबंधित क्षेत्र, उस सभ्यता को समझने के लिए ज्ञान की शक्तिशाली कुंजी हैं।
Author : नीना बंसल, सह आचार्या, राजनीति विज्ञान विभाग, कमला नेहरू काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.4
Price: 251
महिला सशक्तीकरण की चुनौतीः नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक आलोचनात्मक अध्ययन
By: शुभ्रा परमार , विजय शंकर चौधरी
Page No : 58-77
Abstract
नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। यह अधिनियम समानता, समावेशिता, और महिलाओं के सशक्तीकरण का समर्थन करता है। यह अधिनियम महिलाओं को पुरुषों के साथ समान अधिकारों और अवसरों की पहुँच प्रदान करता है। यह अधिनियम समाज के अलग-अलग वर्गों, जातियों, और समुदायों में महिलाओं की समावेशिता को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य है समाज के हर वर्ग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि समाज समृद्ध हो सके। इस अधिनियम के माध्यम से समाज में एक समरस, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना की जा सकती है, जहाँ हर व्यक्ति को उसकी क्षमताओं और प्रतिभा के आधार पर समान अवसर प्राप्त हो सके। प्रस्तुत शोध-आलेख में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा इस अधिनियम से भारत की महिलाएं किस प्रकार लाभान्वित हो सकती हैं उसकी समीक्षा की जाएगी।
Authors:
डॉ. शुभ्रा परमार : सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
विजय शंकर चौधरी : शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.5
Price: 251
भारत में लोकलुभावन राजनीति एवं संसदीय लोकतंत्रा की गतिशीलता
By: अंशु कुमार
Page No : 78-96
Abstract
यह शोधपत्र भारत में लोकलुभावनवाद और संसदीय लोकतंत्र के बीच के संबंधों को प्रस्तुत करता है। लोकलुभावनवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो अभिजात्य वर्ग के विरूद्ध आम जनता और उनके हितों पर ध्यान केन्द्रित करती है। आजादी के बाद से लोकलुभावनवाद राजनीति में भारत एक प्रभावशाली शक्ति रहा है। विभिन्न दलों के नेता जनता से अपील करने के लिए लोकलुभावनवादी भाषणों का प्रयोग करते हैं। उपलब्ध साहित्य और केस स्टडीज के आधार पर, यह शोधपत्र तर्क देता है कि लोकलुभावनवादी शासन व्यवस्था संभावित रूप से संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत को कमजोर कर सकती है, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन आदि। हालाँकि, भारत में लोकलुभावनवाद के उदय ने राज्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में भी चिंता बढ़ा दी है। यह शोधपत्र लोकलुभावनवाद, लोकलुभावनवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और भारत के संसदीय लोकतंत्र पर लोकलुभावनवाद के प्रभाव पर हुए बहसों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और उन चुनौतियों का पता लगाता है जिनका देश को इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने में सामना करना पड़ता है।
Author : श्री अंशु कुमार, पीएच. डी. स्कॉलर, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली। और सहायक आचार्य, आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.6
Price: 251
By: शरद कुमार यादव
Page No : 97-115
Abstract
भारत की प्रगतिशील विकास गाथा में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात किया जाता है। यह उद्योग रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत भी है। हालांकि, खनन गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण असमान रहा है। खनन क्षेत्रों में असुरक्षित खनन प्रथाओं, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और स्थानीय समुदायों की अनदेखी के कारण अक्सर स्थानीय निवासियों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। नतीजन, खनन गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं समावेशी विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार ने खनन से प्रभावित समुदायों को उचित लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) शुरू की है, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन (डी.एम.एफ.) के तहत लागू किया जा रहा है। उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में, यह आलेख पी.एम.के.के.वाई. और डी.एम.एफ. योजनाओं के कार्यान्वयन, उनकी चुनौतियों और संभावित समाधानों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों के गहन विश्लेषण के आधार पर, यह आलेख एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
Author: डा. शरद कुमार यादव, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.7
Price: 251
जाति-जनित वैचारिक बहस एवं उनका पुनरीक्षणः सावरकर एवं अंबेडकर की प्रासंगिकता
By: आलोक कुमार गुप्ता , संजय कुमार अग्रवाल
Page No : 116-132
Abstract
यह शोध पत्र हिंदू समाज के भीतर जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए विनायक दामोदर सावरकर और भीमराव रामजी अंबेडकर के विपरीत दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है। रत्नागिरी में सावरकर के व्यावहारिक सुधारों का उद्देश्य अंतर-जातीय भोजन, विवाह और धार्मिक और शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंँच के माध्यम से जाति की बाधाओं को खत्म करना था। उनके प्रयासों ने सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर के हस्तक्षेप की क्षमता पर प्रकाश डाला, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक मुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। इसके विपरीत, हिंदू धर्म की जडे़ जमाई जाति व्यवस्था से मोहभंग हो चुके आंबेडकर ने इसे पूरी तरह से त्यागने और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की वकालत की, जिसे उन्होंने एक अधिक समतावादी विकल्प के रूप में देखा। अपनी अलग-अलग रणनीतियों के बावजूद, दोनों नेताओं ने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामाजिक न्याय और उत्थान का एक साझा लक्ष्य साझा किया। यह अध्ययन सावरकर के तर्कवादी परिप्रेक्ष्य में तल्लीन करता है, जिसने अस्पृश्यता को मिटाने के प्रयासों के साथ हिंदू धर्म के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता और जाति व्यवस्था के खिलाफ अंबेडकर की अथक लड़ाई को जोड़ा, जिसकी परिणति उनके ऐतिहासिक रूपांतरण में हुई। यह शोध पत्र भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है, जो समानता और न्याय की खोज में उनकी स्थायी विरासत को दर्शाता है।
Authors:
डॉ. आलोक कुमार गुप्ता : सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग एवं लोक प्रशासन विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, चेरी-मनातू, रांची।
डॉ. संजय कुमार अग्रवाल : सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, चेरी-मनातू, रांची।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.8
Price: 251
उपाश्रित जनजातीय विकास में पेसा अधिनियम का विश्लेषणात्मक अध्ययन: राजस्थान के संदर्भ में
By: शिव कुमार मीणा
Page No : 133-144
Abstract
उपाश्रित यानि समाज का कमजोर व दलित वर्ग। यह वर्ग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी रूपों में शेष समाज से काफी पिछड़ा है। इस वर्ग को विकास के प्रयासों व योजनाओं में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। स्वतत्रंता के बाद भारतीय समाज में उपाश्रित वर्ग (अनुसूचित जनजातियों) के सामने गरीबी, स्वास्थय, अशिक्षा, पिछड़ापन, विस्थापन आदि अनेक समस्याएं थी। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुसूची 5 शामिल की। जिसने अनुसूचित जनजातियों के विकास के रास्ते खोले। इसी क्रम में पेसा अधिनियम 1996 पारित किया गया। जो उपाश्रित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों) को स्थानीय स्वशासन का अधिकार देता है। प्रस्तुत शोध में इस अधिनियम का ही राजस्थान के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।
Author : श्री शिव कुमार मीणा, पी.एच.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.9
Price: 251
बैगा जनजातियों का सामाजिक जीवन एवं समस्याएं: एक समाजशास्त्राीय अध्ययन
By: दीपक कुमार खरवार , विभूति भूषण मलिक
Page No : 145-163
Abstract
सदियों से आदिवासी समाज प्राकृतिक परिवेश में रहते रहे हैं एवं अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं जिसके कारण इनकी अपनी एक अलग संस्कृति विकसित हो गयी हैं। शायद इसलिए आदिवासियों एवं पर्यावरण के बीच एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता हैं, (सरकार एवं दासगुप्ता, 2000)। लेकिन विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण इनके सामाजिक जीवन पद्धति में परिवर्तन होने लगा है। बैगा समुदाय की सामाजिक संरचना काफी पुरानी और अनूठी है। उनकी यह व्यवस्था अपने अनोखेपन के साथ अभी तक चल रही है। समय-समय पर दूसरे समुदायों द्वारा कई तरह के हस्तक्षेप का सामना करने के बावजूद बैगा समुदाय अपनी परम्पराओं के साथ जीवन-यापन कर रहा है। लेकिन समय के साथ उनके सामाजिक जीवन में अब परिवर्तन होने लगा है। बैगा समुदाय से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से पता चलता है कि यह समुदाय अब गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी सुविधाओं से वंचित है और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है।
प्रस्तुत शोध पत्री बैगा जनजातियों का सामाजिक जीवन एवं समस्याएं: एक समाजशास्त्रीय अध्ययनी में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की बैगा जनजातियों के सामाजिक जीवन एवं उनके समक्ष मौजूद समस्याओं के विश्लेषण पर आधारित है। इस शोध पत्र में प्राथमिक तथ्यों के आधार पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से यह जानने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता के सात दशक बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब आधुनिकता के इस दौर में बैंगा जनजातीय समुदाय की सामाजिक जीवन एवं उनके स्थितियों में कितना सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह शोध पत्र बैंगा जनजातीय समुदाय और विकास के इस क्रम में उनके सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है को नए परिप्रेक्ष्य से समझने में सहायक होगा।
Authors:
डाॅ. दीपक कुमार खरवार, पोस्ट-डाक्टरल फेलो (ICSSR), समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ।
प्रो. विभूति भूषण मलिक, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.02.10
Price: 251
Jul- to Sep-2024
By: प्रो. अशोक विशनदास
Page No : v-vi
साइबर सुरक्षा एवं भारत सरकार की नीतियों का अध्ययनः अवसर एवं चुनौतियां
By: लुके कुमारी , विजय दीक्षित
Page No : 1-16
Abstract
साइबर सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के रणनीतिक विषयों में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर राज्य और गैर-राज्य प्रायोजित साइबर हमलों में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत ने रक्षा, आर्थिक, संचार, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें किसी भी साइबर हमलों से सुरक्षित किया जा सके। इसलिए भारत सरकार के छह मंत्रालयों और प्रधान मंत्री के शीर्ष कार्यालय ने सुरक्षा के लिए सक्रिय जिम्मेदारियां ली हैं। हाल के एक या दो दशकों में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीतियों, कानून, मानकों, संस्थानों, सहयोग और पदों जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के विकास सहित कई उपाय किए हैं। भारतीय विधानमंडल किसी भी क़ानून में साइबर अपराध को परिभाषित नहीं करता है। यहांँ तक कि 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, जो साइबर अपराध से संबंधित है, इस शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हालाँकि सामान्य तौर पर, साइबर अपराध इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से या उसकी सहायता से की गई किसी भी आपराधिक गतिविधि को संदर्भित करता है।
Authors
लुके कुमारी : सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, भारती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
विजय दीक्षित : विजय दीक्षित, शोधार्थी, एस. डी (पी जी) कॉलेज, गाजियाबाद।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.1
Price: 251
डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षाः मुद्दे और चुनौतियाँ
By: अभय प्रसाद सिंह , कृष्ण मुरारी
Page No : 17-31
Abstract
भूमंडलीकरण के इस दौर में जहाँ दुनियाँ के देशों में उत्तरोतर संपर्क ने उनके अंतर्संबंधों को संबल दिया है वहीं इन्टरनेट के माध्यम से डेटा अंतरण ने डेटा सुरक्षा को संवेदनशील बनाया है। इससे छुटकारा पाने में साइबर सुरक्षा एवं व्यक्तिगत डेटा और गैर-व्यक्तिगत डेटा नियमन महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आए हैं जिसके औपचारिक और अनौपचारिक आयाम विचारणीय हैं। साइबर सुरक्षा में डिजिटल नेटवर्क और प्रोग्राम को डिजिटल हमलों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जिससे डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बरकरार रहे। सम्प्रति, साइबर सुरक्षा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह निजता एवं संसाधन के व्यक्तिगत डेटा स्वामित्व के क्षेत्र में अतिक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी योजनाओं में लोगों के व्यक्तिगत और निजी आकड़ों को डिजिटल माध्यमों से संग्रहित किया जाने लगा ताकि सरकारी नीतियों को अधिक जनोपयोगी बनाया जा सके। इस आलेख में व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा और वित्तीय संस्थायों में प्रयुक्त डेटा से संबंधित चुनौतियों, मुद्दों एवं न्यायिक और नीतिगत समाधानों का शोध अन्वेषण प्रस्तुत किया गया है।
Authors :
अभय प्रसाद सिंह : प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
कृष्ण मुरारी : असिस्टेंट प्राफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.2
Price: 251
भारत में साइबर अपराध: प्रवृत्तियाँ, विश्लेषण एवं समाधान
By: चंदन सिंह , प्रदीप कुमार सिंह
Page No : 32-51
Abstract
आज के आधुनिक डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी के प्रसार ने हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हालांकि बढ़ी हुई संयोजकता और डिजिटलीकरण के लाभों के साथ-साथ साइबर अपराध में एक व्यापक और उभरती चुनौती भी है। साइबर अपराध में डिजिटल चैनलों के माध्यम से की जाने वाली अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो दुनिया भर में व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती है। वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी से लेकर ऑनलाइन उत्पीड़न और डेटा उल्लंघनों तक साइबर अपराधी व्यक्तिगत लाभ के लिए डिजिटल तंत्र की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जिससे आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठा की क्षति और सामाजिक क्षति होती है।
इस शोध पत्र का उद्देश्य साइबर अपराध की प्रवृत्तियों का व्यापक विश्लेषण करना है जो डिजिटल खतरों की विकसित हों रही प्रकृति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर तथा उसके प्रभाव पर प्रकाश डालना है। यह शोध- पत्र बच्चों, महिलाओं और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ साइबर अपराध के रूझानों की जाँच करके,इन रूझानों को चलाने वाले अंतर्निहित कारकों को स्पष्ट करने और साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए संभावित रणनीतियों का पता लगाने का प्रयास करता है।
Authors
डाॅ. चन्दन सिंह : सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय महाविद्यालय, उकलाना, हिसार।
डाॅ. प्रदीप कुमार सिंह : सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, विश्वविद्यालय, लखनऊ।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.3
Price: 251
By: आमना मिर्जा , भावनाथ झा
Page No : 52-63
Abstract
अभिशासन (Governance) द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के अनुप्रयोग कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय तंत्रों में सुधार एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसका अत्यंत व्यापक रूप इस अध्ययन में विश्लेषित किया गया हैं। आईसीटी साधनों जैसे कि निगरानी कैमरे, मोबाइल एप्लिकेशन, और डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म का उपयोग करके न्याय संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा लाॅन्च किया गया ‘हिम्मत ऐप’ प्रयुक्त संदर्भ में काफी प्रासंगिक माना जा सकता है। इस अध्ययन के माध्यम से, प्रौद्योगिकी को पारंपरिक न्याय तंत्रों में एकीकृत करने की जटिल गतिविधियों और प्रभावों का गहन अवलोकन किया गया है ताकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
Authors :
डाॅ. आमना मिर्जा : सह आचार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
डाॅ. भावनाथ झा : सहायक आचार्य, आत्माराम सनातन ध्ार्म काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.4
Price: 251
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर सुरक्षाः सुशासन के परिप्रेक्ष्य में
By: मीना रानी
Page No : 64-77
Abstract
इंटरनेट सेवाओं के तेजी से विकास के कारण साइबर हमलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साइबर खतरे अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं और स्वचालन, सुरक्षा को अप्रभावी बना देता है। पारंपरिक साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण का नए साइबर खतरों से लड़ने पर सीमित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, हमें नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर अपराध से निपटने में सहायता कर सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र में साइबर सुरक्षा में प्रयुक्त की जा रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकें एवं उनकी क्षमताओं की विवेचना का प्रयास किया गया है। साथ ही यह शोध कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों की सीमाओं पर भी प्रकाश डालता है। यह शोध इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर खतरों की पहचान, उनकी भविष्यवाणी और डेटा संचालित द्वारा इन मूल्यों की रक्षा करने का अवसर प्रस्तुत करता है।
Author :
मीना रानी : सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.5
Price: 251
साइबर अपराध और युवाः भारतीय सन्दर्भ में विश्लेषण
By: प्रवीन कुमार झा , विनायक राय , संगीता
Page No : 78-91
Abstract
तकनीकी प्रगति ने समाज में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं, लेकिन उन्होंने नए प्रकार के आपराधिक अवसर भी पैदा किए हैं। हाल के वर्षो में साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के मुद्दे तेजी से बढ़े हैं, जिससे जांँच की एक नई उपशाखा (Cyber Crime Cell) को जन्म दिया है। यह शोध कार्य साइबर अपराधों के अर्थ और संभाव्यता तथा लक्षित पीड़ितों, मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का इतना अहम् हिस्सा बन गया है कि इसके बिना जीना लगभग असंभव है। भारतीय युवा सोशल नेटवर्किं ग पर जितना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, उससे उनके जीवन में इसका महत्व तो पता चलता है, लेकिन क्या उन्हें सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी साझा करने की गंभीरता का एहसास है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यह शोध यह जानने का प्रयास करता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स युवाओं के जीवन में किस तरह से प्रवेश कर रही हैं और उनके जीवन और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिससे साइब अपराध को बढ़ावा मिलता है। इन सब को समझने के बाद, यह शोध पत्र यह भी सुझाव देता है कि इन्हें कैसे रोका और प्रतिबंधित किया जा सकता है।
Authors :
प्रवीन कुमार झा : प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
विनायक राय : दिल्ली विश्वविद्यालय।
संगीता : प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.6
Price: 251
भारत में साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा संरक्षण
By: लक्ष्मी परेवा
Page No : 92-100
Abstract
जब सूचना प्रबंधन के क्षेत्र की बात आती है, तो साइबर सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है अपनी जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। हालाँकि, साइबर सुरक्षा का सटीक वर्णन करना कठिन है, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक महत्वपूर्ण धारणा है। इसके अतिरिक्त, अतीत में, इसे निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करना, सूचना विनिमय और गुमनामी जैसी अन्य अवधारणाओं के साथ भ्रमित किया गया है। हाल के वर्षों में लगातार बढ़ते आईसीटी बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, और ऐसा करने के लिए एक डेटा सुरक्षा ढाँचा व्यावहारिक रूप से आवश्यक है। इंटरनेट में हमेशा बदलाव होता रहता है, यही इसके पीछे का कारण है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का बुनियादी ढाँचा एक आवश्यक घटक है क्योंकि यह सभी आवश्यक राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे के बीच संपर्क लिंक के रूप में कार्य करता है। जैसे.जैसे अधिक से अधिक देश ई.गवर्नेंस और ई.कॉमर्स पहल शुरू करते हैं, एक विश्वसनीय साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे मॉडल की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। आज के सूचना युग में, लगातार विकसित हो रहे आईसीटी बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा वास्तुकला की आवश्यकता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देश के बुनियादी ढांचे की रीढ़ डेटा और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य रूपों के आदान-प्रदान और प्राप्त करने की प्रणाली है। पहले एक ठोस साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की स्थापना के बिना दुनिया में कहीं भी ई-गवर्नेंस या ई-कॉमर्स संचालित करना असंभव है। यह लेख इस बुनियादी ढाँचे का सारांश देगा और फिर हम जो उम्मीद कर सकते हैं उसके आधार पर भारतीय संदर्भ में इससे निकलने वाले पैटर्न और अनिवार्यताओं के बारे में बात करेंगे।
Author :
डा. लक्ष्मी परेवा : सहायक आचार्या, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.7
Price: 251
साइबर-अपराध भारत के साइबर परिदृश्य में एक उभरता हुआ खतरा
By: शालिनी प्रसाद , अभय कुमार
Page No : 101-116
Abstract
आज की दुनिया में सुरक्षा की अवधारणा तेजी से बदलती जा रही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनियंत्रित प्रसार ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने में कई चिंताएँ पैदा कर दी हैं। साइबर-अपराध अब एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है और साइबर स्पेस में उन खतरों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो सभी को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में, इस लेख का उद्देश्य साइबर अपराध की अवधारणाओं और अर्थ को समझना है। इसके अलावा, शोध का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ‘‘साइबर अपराध‘‘ के प्रतिकूल प्रभाव की जांच करना है। यह उन खतरों और चुनौतियों का वर्णन करता है जिनका भारत का साइबर स्पेस सामना कर रहा है, या भविष्य में सामना करने की संभावना है। यह लेख इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि भविष्य में साइबर अपराध एक बड़ा खतरा कैसे बन सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पहलें अपनाई गई हैं। यह अध्ययन उन विभिन्न पहलों और नीतियों का विश्लेषण करेगा, जिन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खतरों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वर्षों से तैयार किया है।
Authors :
डॉ शालिनी प्रसाद : सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
डॉ अभय कुमार : सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.8
Price: 251
शिक्षा और साइबर सुरक्षाः निहितार्थ एवं चुनौतियाँ
By: एकता मीना
Page No : 117-127
Abstract
शिक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ते एकीकरण के साथ, साइबर सुरक्षा दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित करके, शैक्षणिक संस्थान एक सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाया जा सकता हैं जो डिजिटल युग के छात्रों में नवाचार एवं सफलता को बढ़ावा देगा। यह शोध पत्र शिक्षा में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और रणनीतियों की जाँच करता है। इसके अतिरिक्त यह पत्र शैक्षणिक संस्थानों पर साइबर खतरों के प्रभाव का पता लगाता है, शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है, और साइबर जोखिमों को कम करने और डिजिटल शिक्षण वातावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिफारिशों को प्रस्तुत करता है।
Author :
डॉ. एकता मीना : सहायक आचार्या, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.9
Price: 251
स्मार्ट सिटी व साइबर सुरक्षा: भारतीय संदर्भ में एक अवलोकन
By: रिंकी
Page No : 128-136
Abstract
वर्तमान परिपेक्ष्य में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों के समाधान के लिए स्मार्ट सिटी के विकास को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि स्मार्ट सिटी संकल्पना को अपनाने से कुशल व बेहतर शहरी वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिससे सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ आधुनिकता के लाभों का अनुभव किया जा सकता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों के बिना स्मार्ट सिटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के समावेशन के द्वारा स्मार्ट सिटी के विकास को समर्थन दिया जा रहा है। परंतु स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने की राह में हमारे सामने साइबर असुरक्षा के रूप में बहुत सी चुनौतियाँ उपस्थित हैं। जो स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांँचे की सुरक्षा व अखंडता को प्रभावित करती हैं। इसी परिपेक्ष्य में भारत में स्मार्ट सिटी के संदर्भ में साइबर सुरक्षा का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। जिससे स्मार्ट सिटी मिशन के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों को संबोधित करते हुए कुछ समाधान सुझाएं जा सके। भारत में स्मार्ट सिटी के लिए योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सुरक्षित शहर व साइबर सुरक्षा नीति व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके लिए कानून, जनता, प्रक्रिया व तकनीक का एक अच्छा संयोजन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
Author :
डॉ. रिंकी : सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.10
Price: 251
भारत में गोपनीयता की अवधारणा का विकास: साइबर युग के विशेष सन्दर्भ में
By: अक्षत पुष्पम , रजनीश राज
Page No : 137-157
Abstract
आज भूमंडलीकरण के दौर में इन्टरनेट के विकास ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। लेकिन आज सब कुछ जहाँ बस एक क्लिक के दूरी पर मौजूद है वहीं साइबर युग के विकास ने कई नई चिंताओं और चुनौतियों को भी जन्म दिया है जिनमें प्रमुख रूप से गोपनीयता का प्रश्न शामिल है। भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की माने तो आए दिन भारत में साइबर अपराध की संख्या बढ़ती जा है। अतः बढ़ रही साइबर आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संग्रहित डेटा का उपयोग केवल उसी उद्देश्य से किया जा रहा है जिसके लिए यह एकत्र किया गया था। इसी संदर्भ में यह आलेख भारत में गोपनीयता और निजता की अवधारणा के विकास को समझते हुए उसके आम जनता पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करता है।
Authors :
अक्षत पुष्पम : सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग , भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
रजनीश राज : शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.11
Price: 251
By: संजीव कुमार
Page No : 158-175
Abstract
साइबर स्पेस एक तरफ जीवन को बहुत सरल बना रहा है, दूसरी तरफ साइबर आधारित आपराधिक घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। साइबर स्पेस न सिर्फ जानकारी, शिक्षा, पहचान, व्यापार, मनोरंजन उपलब्ध कराने में मदद करता है, बल्कि वर्चुअल सेक्स और हत्याएं जैसी अमानवीय घटनाओं का माध्यम भी बन रहा है। साइबर विशेषज्ञों एवं अन्य शोध के अनुसार कोविड-19 के बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से किशोर लड़कियो के खिलाफ होने वाले इंटरनेट आधारित साइबर अपराध जैसे अपमानजनक टिप्पणी करना, अश्लील संदेश भेजना, जानबूझ कर महिलाओं के फोटो को नग्नावस्था में संलग्न करना आदि है।
यह लेख महिलाओं के प्रति होने वाले इस प्रकार के अपराध के कारण, उसकी प्रवृत्ति और पड़ने वाले प्रभाव को जानने एवं समझने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से सहयोग प्राप्त शोध-कार्य पर आधारित है। इस शोध-कार्य का शीर्षक “महिलाओं के लिए साइबर स्पेस में चुनौतियाँ 2020-21 में दिल्ली और एनसीआर के चुनिंदा क्षेत्रों का एक अध्ययन” था। इस शोध के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल 13 जिलों का अध्ययन किया गया है। इन जिलों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त उत्तरदाताओं के अनुभवों एवं आंकड़ो का गहन विश्लेषण किया गया है। साथ ही साइबर संबंधित अपराधों के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा किए गए कानूनी प्रावधानो और उसकी प्रभावशीलता का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
Author :
डॉ संजीव कुमार : सहायक प्राध्यापक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.12
Price: 251
सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली में साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता की चुनौतियाँ एवं समाधान
By: शशि भूषण
Page No : 176-196
Abstract
वर्तमान डिजिटल युग में, रिमोट सेंसिंग (RS) और भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो डेटा संग्रह, विश्लेषण और भंडारण की नई संभावनाएँ प्रस्तुत करता है।हालांकि, इन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की चिंताएँ भी महत्त्वपूर्ण हो गई हैं। सुदूर संवेदन अथवा रिमोट सेंसिंग (RS) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के एकीकरण से स्थानिक डेटा विश्लेषण में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए शक्तिशाली उपकरण उपलब्ध हुए हैं। हालांकि, इस एकीकरण के साथ-साथ कई साइबर सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न होते हैं। यह पेपर RS और GIS से संबंधित साइबर सुरक्षा चुनौतियों की जाँच करता है, जिसमें डेटा की अखंडता, उपलब्धता और गोपनीयता शामिल हैं।
यह शोध-पत्र विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों और कमजोरियों की पहचान करता है, जिनसे RS और GIS प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती हैं। इनमें डेटा ब्रीच, साइबर हमले, मैलवेयर, और अन्य सुरक्षा खतरों का विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, यह अध्ययन उन मौजूदा सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करता है जिन्हें इन खतरों से बचने के लिए लागू किया जा सकता है। इसमें डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ, और नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे उपाय शामिल हैं।
यह शोध-पत्र उभरती तकनीकों और उनके सुरक्षा पर प्रभावों पर भी चर्चा करता है। नई तकनीकों का विकास, जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है, लेकिन इन तकनीकों के उपयोग में भी नई चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। केस स्टडीज और सुझावों के माध्यम से, यह शोध-पत्र RS और GIS प्रणालियों की साइबर सुरक्षा की गहन समझ प्रदान करता है और संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ पेश करता है।
अंततः, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि RS और GIS में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। इस दिशा में निरंतर शोध और उन्नत तकनीकों का विकास आवश्यक है, ताकि इन प्रणालियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
Author :
डाॅ. शशि भूषण : वैज्ञानिक, पर्यावरण शोध एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2024.16.03.13
Price: 251
By: मीना मिश्रा
Page No : 197-200
Price: 251
Jan- to Mar-2023
सम्पादकीय
सुशासन: सहभागिता, जवाबदेही और पारदर्शिता
By: ..
By: विजय शकंर चैधरी
Page No : 1-14
Abstract
सारांशः प्रस्तुत आलेख ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में संघवाद के बदलते आयामों का विश्लेषण करता है। संघवाद की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम,1935 से र्हुइ । संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्तिको साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है।आजादी के उपरांत से लेकर अब तक भारतीय संघवाद का स्वरूप बदलता रहा है।भारतीय राजनीति में र्कइ ऐसे परिवर्तन हुए जिसने संघीय प्रणाली को कई स्तरों पर प्रभावित किया है। इसके कारण देश में संघवाद के अलग-अलग चरण देखने को मिलते हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ‘एकदलीय प्रभुत्व’ के दौरान ‘केंद्रीकृत संघवाद’ था।
राजनीतिक एकल सत्ता और समय की माँग ने एक ऐसे परिस्थिति निर्मित की कि जनता के सामने ध्रुवतारा के रूप में नरेन्द्र मोदी आए और वर्ष 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सौदेबाजी व्यवस्था का वस्तुतः अंत कर दिया। गठबंधन की राजनीति चलती रही लेकिन सौदेबाजी बिल्कुल नियंत्रण में रही। इस सरकार ने अनुच्छेद 356 का कम दुरुपयागे किया। 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ठासे रूप से सत्ता में है। इसके फलस्वरूप केंद्र राज्यों के मुकाबले और मजबूत हो गया। 2014 के बाद पुनः केंद्रीकरण की प्रवृतियाँ मजबूत होने लगी हैं। जीएसटी, नीति आयोग, एनआईए (NIA) एवं कोरोना महामारी के विरूद्ध संघर्ष के कारण केंद्र की महती भूमिका हो गई है।
Author :
विजय शकंर चैधरी : शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।
Price: 251
भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा के समक्ष सीखने का अनुकूलतम वातावरणः सन्दर्भ एवं चुनौतियाँ
By: कुमारी रितु सिंह
Page No : 15-24
Abstract
मनुष्य में सीखने की उत्कट प्रवृत्ति उसे सभी सजीवों में विशिष्टतम स्थान प्रदान करती है। सीखना एक जीवन-पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका संपादन विभिन्न चरणों, प्रक्रियाओं एवं परिस्थितियों में होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से संपादित होती है। व्यक्ति के सीखने की व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध क्रिया औपचारिक परिवेश एवं वातावरण में संपादित होती है तथा व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सीखने के अनौपचारिक परिवेश एवं वातावरण में फलीभूत होती है। सीखने की प्रक्रिया को व्यक्ति औपचारिक रूप से एवं संज्ञानात्मक ढंग से कुछ समूह, संस्थाओं एवं निकायों की सहायता से संपादित करता है। इसमें प्रमुख रूप से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएं आती हैं। वहीं अनौपचारिक शिक्षण में परिवार, साथी, समहू , समुदाय, सांस्कृतिक समूह एवं समस्त सामाजिक क्रियाओं- अनुक्रियाऔ को रखा जा सकता है जो संज्ञानात्मक या गैर-संज्ञानात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया को संपादित करती रहती है ।
Author :
कुमारी रितु सिंह : शोधार्थी, (पी.एच.डी.) महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।
Price: 251
भारत में सकारात्मक कार्यवाही और आरक्षण
By: अरविन्द कुमार यादव
Page No : 25-58
Abstract
भारत में कई दशकों से सकारात्मक कार्र वाई नीति के तहत समाज के उपेक्षित वर्गो को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। सरकार ने उपेक्षित वर्गो के चहुँमुखी विकास के लिए सामाजिक न्याय के तहत अनेक लक्ष्य निर्धारित किए है जिसमें उनके समावेशीकरण करने के लिए अनेक नीतियां प्रमुख है। भारतीय समाज के उपेक्षितों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि आरक्षित वर्गों का सामाजिक, आर्थिकं और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर किया जा सके । संविधान का यह लक्ष्योन्मुख प्रावधान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । प्रस्तुत शोध -पत्र में आरक्षित समुदायों के ऊपर आरक्षण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को विभिन्न तथ्यों एवं की सहायता से समीक्षा की गई है ।
Author :
अरविन्द कुमार यादव : सहआचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, डा0 भीम राव अम्बेडकर महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
Price: 251
भारत में ई-कॉमर्स बनाम भौतिक खुदरा स्टोरः एक तुलनात्मक अध्ययन
By: जगदीप सिंह , ममता कुमारी
Page No : 59-72
Abstract
उपभोक्ताओं का ध्यान पारंपरिक वितरण चैनलों से हटकर ऑनलाइन/ई-कॉमर्स वितरण चैनलों की ओर जा रहा है, जो पारंपरिक और केवल-क्लिक चैनलों का एक मिश्रण है। इंटरनेट विशेष रूप से ई-कॉमर्स ने वाणिज्यिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है। ई-कॉमर्स पहले कुछ सेवाओं जैसे एयरलाइन टिकट, ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग, ऑनलाइन सेल-फोन रिचार्जिंग आदि तक सीमित था। हाल ही में, ई-कॉमर्स ने खुदरा और किराना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। अधिकांश व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं क्योंकि वो घर बैठे खरीददारी कर सकते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता का प्रभाव सब्जियों, किराना या दोनों के लिए क्रय निर्णयों को प्रभावित करता है। यह भी पता चला है कि स्थानीय दुकानों की तुलना मे इंटरनेट की कीमतें काफी कम है। हालांकि हम स्थानीय कंपनियों के साथ सौदेबाज़ी कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय व्यापारियों और इंटरनेट पोर्टलों के बीच कीमतों में काफी असमानता है। ई-कॉमर्स बाजार को व्यापक बनाने के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओ और ग्राहकों को एक मंच पर एक साथ लाने का प्रयास करता है। यहां तक कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स और कई अन्य जैसे बड़े निगम स्थानीय किराना डीलरों को अपने वेब पोर्टलो के माध्यम से बेचने के लिए उत्तरोत्तर प्रोत्साहित कर रह हैं; फिर भी, उनमें से कई जागरूकता की कमी और तकनीकी कठिनाइयों के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। अध्ययन में पाया गया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटो पर कीमतें छोटे किराना स्टोर (स्थानीय खुदरा विक्रेताओं) की कीमतों की तुलना में काफी कम है, लेकिन स्थानीय किराना दुकानों मं सौदेबाजी संभव है। छोटी किराना दुकानों और ई-कॉमर्स वेबसाइटो या इंटरनेट पोर्टल के बीच, कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर और कटौती होती है।
Author :
जगदीप सिंह : प्रोपराइटर रीकैप कंसल्टेंसी एंड जनरल सप्लाई धोराजी , राजकोट, गुजरात।
ममता कुमारी : के.वी.के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, पिपलिया, राजकोट, गुजरात।
Price: 251
भारतीय श्रमिक आंदोलन के समक्ष चुनौतियाँः अतीत से वर्तमान तक
By: डा0 रूणा आनंद
Page No : 73-89
Abstract
श्रमिक आंदोलन का विकास स्वतत्रंता पूर्व ब्रिटिश शासन, भारतीय राजनैतिक विचारधारा एवं विश्व-पटल पर होने वाले श्रमिक आंदोलनो या परिवर्तनों से प्रभावित था। कालांतर में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर श्रमिक आंदोलनो के द्वारा, राज्य की ओर से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। श्रमिक आंदोलन की सफलता राज्य और पूंजीपतियो द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। मुख्यतः यह आंदोलन श्रम, पूंजी और सरकार के अन्यान्याश्रित संबंध पर निर्भर है। श्रमिक अपने श्रम से पूंजी निर्माण करते है और उस पूंजी में संतोषजनक भाग मिलने की उम्मीद करते है। राज्य से उन्हें यह अपेक्षा रहती है कि, राज्य उनके मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों कि रक्षा कर संरक्षण और संवर्धन में भी सहयोग करें। राज्य, श्रम और पूंजी के इस संबंध ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, मुख्य रूप से उदारीकरण और वैश्वीकरण के समय श्रमिक आंदोलन के स्वरूपों और उदेश्यो को अत्याधिक प्रभावित किया है। यह शोध -पत्र सिर्फ औपचारिक श्रमिकों तक सीमित है। जिनका विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन किया गया है लेकिन वर्तमान में अनौपचारिक श्रमिकों के आंदोलन की बदलती भूमिका के कारण यथायोग्य अति संक्षिप्त में उन पर भी प्रकाश डाला गया है।
Author :
डा0 रूणा आनंद : सहायक आचार्या, अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, वैशाली महिला कॉलेज, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बिहार।
Price: 251
गाँधी जी एवं समावेशी विकास का सशक्त आधारः सर्वोदय
By: डा0 संतोष कुमार सिंह
Page No : 90-103
Abstract
समावेशी विकास एक बहुआयामी सिद्धान्त है, जो सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय तथा सम्यक न्याय पर आधारित है। यह सिद्धान्त अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, जिससे व्यक्ति अपने कौशल विकास के माध्यम से राष्ट्र में अपनी सशक्त भागीदारी निभा सके। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गो के लिए बुनियादी सुविधाओं के प्रदान करने के साथ गरिमामयी जीवन जीने के साधनो का विकास तलाश करता है। समावेशी विकास का उद्देश्य एक ऐसे राज्य का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विकास हो सके। समावेशी विकास की संकल्पना गरीबी उन्मूलन के पारम्परिक उद्देश्य से भी ऊपर उठकर समाज के वंचित और पिछडे़ वर्गों का सशक्तिकरण करना है। इस द्रिष्टि से भारत के पास गाँधी जी का अनुकरण करने और उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जो संदेश दिया, उसे बिना अतिरिक्त प्रयास के प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्हें बहुत पहले ही इस बात का अहसास हो गया था कि भारत को भविष्य में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने इस देश को हमेशा के लिए महान और गौरवशाली राष्ट्र बनाए रखने के लिए समावेशी विकास का एक माॅडल ‘सर्वोदय‘ प्रस्तुत किया। समावेशी विकास के रूप में गाँधी जी द्वारा वर्णित सर्वोदय ही वह विचार है जो सबके कल्याण को परिभाषित करता है। अथार्थ वेश्विक परिद्र्श्य से इसका आशय लिया जाए तो इस द्रिष्टिकोड से सभी का उदय हो और जिससे सभी का सर्वागीढ विकास हो सके। सर्वोदय सिद्धान्त में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है और यह “वसुधैव कुटुम्बकम्” की अवधारणा को सशक्त बनाती है। सही अर्थो में सर्वोदय ही वह सिद्धान्त है जो समावेशी विकास के समस्त आयामों को स्पर्श करता है ।
Author :
डा0 संतोष कुमार सिंह : सहायक आचार्य, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड।
Price: 251
शिक्षा नीति एवं शिक्षानीति की प्रासगिकता
By: कु0 वीणा कुमारी , डा0 गजानंद सिंह
Page No : 104-112
Abstract
किसी भी समाज या देश की प्रगति में शिक्षा का धुरीय महत्व होता है। भारतीय शिक्षा कामोबेश मेकाॅले की विरासत को आज भी ढो रही है। परन्तु उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज जरूरत है एक आवश्यकता एवं कौशल आधारित शिक्षा की जो भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। साथ ही इसमें महिलाओं के मानवाधिकारों की संरक्षा के उत्क्रम भी हो क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को उचित-अनुचित, नैतिक-अनैतिक आदि मूलयो का ज्ञान करवाती है तथा अपने अधिकार व कर्तव्यो का बोध करवाती है जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत आलेख प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकारो के आलोक में वर्तमान शिक्षा नीति 2020 के परीक्षण का एक प्रयास है। प्रस्तुत अनुशीलन से यह उजागर होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तरह महिलाओ के शिक्षा संबंधी अधिकारो के अनुरूप है।
Authors :
कु0 वीणा कुमारी : शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, जी.बी. काॅलेज, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार।
डा0 गजानंद सिंह : आचार्य, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, रामगढ़ कैमूर , बिहार।
Price: 251
विश्व आधिपत्य की लालसाः यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की अवांछनीय भूमिका
By: डा0 पकंज लखेरा
Page No : 113-124
Abstract
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख घटनाओं में से एक है। यह वैश्विक तनाव पैदा कर रहा है, हथियारो की होड़ बढ़ा रहा है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों मे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और यहां तक कि परमाणु संघर्ष में भी समाप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से यह न केवल युद्धरत राष्ट्रों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आपदा होगी। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में तेल, प्राकृतिक गैस, खाद्यान्न, मोटल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आ रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन इन सभी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप दुनिया के विभिन्न हिस्सो में धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती गरीबी और बढ़ती भूख हो अवश्यंभावी है। संक्षेप में कहें तो युद्ध विश्व व्यवस्था को काफी हद तक बदल सकता है। यूक्रेन वस्तुतः एक युद्ध का मैदान बन गया है जहाँ दुनिया की प्रमुख शक्तियाँ अपनी सेन्यें तकनीकी शक्ति का प्रदर्श न कर रही हैं। सामान्यतया, नाटो में शामिल होने या न होने के लिए यूक्रेनी संप्रभुता के सवाल पर युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन, पूरी स्थिति का गहन विश्लेषण एक अलग तस्वीर पेश करता है। एक युद्ध जो रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देने के लिए लड़ रहा है, एक युद्ध जो यूक्रेन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए जारी किए हुए है, एक युद्ध जिसे अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर प्रायोजित कर रहा है। एक ऐसा युद्ध जहां अमेरिका केवल अपने राष्ट्रीय हितो को देख रहा है और पूरी दुनिया को दांव पर लगा दिया है । यह शोध पत्र वर्तमान स्थिति में अमेरिका की भूि मका का विश्लेषण करना चाहता है। क्या अमेरिका लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है या वह सिर्फ रूस को कमजोर करना चाहता है और युद्ध के बढ़ने के माध्यम से अपना विश्व आधिपत्य जारी रखना चाहता है? क्या अमेरिका के लिए यह बुद्धिमानी होगी कि वह रूस पर अधिक ध्यान केंद्रित करे और उस वास्तविक चुनौती को नजरअंदाज करे जो बढ़ते चीन के रूप में है?
Author :
डा0 पकंज लखेरा : सहआचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी श्रद्धानंद काॅलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
Price: 251
हरियाणा पंचायती राज चुनाव एवं निर्वाचन पात्राता शर्तें: एक अध्ययन
By: डा0 सुमन लता , डा0 अजीत कुमार
Page No : 125-138
Abstract
पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की आधार व ग्रामीण विकास की धुरी है। प्राचीन काल से ही परम्परा व भाईचारा पंचायतो का इतिहास रहा है इसी संदर्भ में सामाजिक मान्यताओं, स्थानीय व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा इनको शक्तियाँ प्रदान की गई इनके निर्णय न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आदि सभी क्षेत्रो में स्वीकार होते हैं इसलिए इनका पालन आत्मीयता से किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने तेजी से और योजनाबद्ध ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न अधिनियमो एवं कार्यक्रमों को लागू किया है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर इन अधिनियमों और कार्यक्रमों को संशॊधित भी किया जाता रहा है ताकि ग्रामीण विकास को गतिमान बनाया जा सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सुधारात्मक प्रयास के रूप में पाचंवें सामान्य पंचायती राज चुनाव में पात्रता शर्तो का निर्धारण किया गया। हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थओ के वर्ष 1994, 2000, 2005, 2010 और 2016 में चुनाव संपन्न हुए है। प्रस्तुत प्रपत्र मे पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव, 2016 में पात्रता शर्तों संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण प्राथमिक और द्वितीय स्त्रोतो पर आधारित है। जिसका मुख्य उद्देश्य पंच, सरपचं और ग्रामीण व्यक्तियो से पाचंवें सामान्य पंचायती राज चुनाव में लागू नवीन पात्रता शर्तो संबंधी द्रिष्टीकोड जानना और पंचायती राज संस्थाओं में सुधार सम्बंधित सुझाव देना है।
Authors :
डा0 सुमन लता : सहायक आचार्या, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)।
डा0 अजीत कुमार : सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज,रोहतक (हरियाणा)।
Price: 251
उत्तराखण्ड की आदिम जनजातिः वनराजी (वनरावत/वनरौत) की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति
By: डा0 घनश्याम जोशी , डा0 दीपक पालीवाल
Page No : 139-148
Abstract
उत्तराखण्ड में मुख्यतः पाचं प्रकार का जनजाति समाज रहता है। जिसमें भोटिया,थारू, जौनसारी, बोक्सा और वनरावत या वनराजी हैं। पहले चार प्रकार की जनजाति समाज अपने प्राकृतिक स्वरूप, परम्पराओं और मान्यताओंके साथ आधुनिक समाज मेंरच-बस गया है। किन्तु एक जनजाति समाज जिसे वनरावत या वनराजी नाम से जाना जाता है, समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर रहा और अल्पतज्ञात के कारण आदिम जनजाति की श्रेणी में बना रहा्। इस शोध-पत्र के माध्यम से आदिम जनजाति, वनरावत का समाज की मुख्य धारा में जुड़ने और इससे उनके सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में आए बदलावो का अध्ययन करना है। यह जनजाति उत्तराखण्ड की अन्य जनजातियों से इस मामले में भिन्न है। इनकी जनसंख्या कुछ सैकड़ों में ही बची है और इनके विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
Authors :
डा0 घनश्याम जोशी : सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड ।
डा0 दीपक पालीवाल : सहप्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
Price: 251
By: डा0 जोरावर सिंह राणावत
Page No : 149-162
Abstract
सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी और सुशासन के लिए सरकारों ने कई प्रयास किए हैं जिनमें समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, नागरिक अधिकार पत्र लागू करना, सूचना का अधिकार जैसे अधिनियम बनाना आदि प्रमुख हैं। इसी क्रम में देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश राज्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान का अधिनियम, 2010 पारित कर सुशासन की नई दिशा दिखाई है जिसका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भी नागरिक अधिकार पत्र विधेयक, 2011 प्रस्तुत कर इस दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तुत लेख में देश में सुशासन हेतु अब तक किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए राज्यों द्वारा लाके सेवा प्रदायगी हेतु पारित किए गए अधिनियमो का तुलनात्मक अध्ययन किया गया हैं और केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अन्त में लोक सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।
Author :
डा0 जोरावर सिंह राणावत : सहायक आचार्य, अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, भीलवाड़ा (राजस्थान), संगम विश्वविद्यालय।
Price: 251
By: Kalpesh B. Panara
Page No : 163-168
Apr- to Jun-2023
By: ..
Page No : v
भारतीय लोकतंत्र में संविधान की केन्द्रियता
By: अभय प्रसाद सिंह , कृष्ण मुरारी , रूपक कुमार
Page No : 1-16
Abstract
इस आलेख का उद्देश्य संविधान में निहित उन मूल्यों को समझना है जिसकी प्रासंगिकता मतदाताओं की आकांक्षाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता के राजनीतिक अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में संवादित है। संविधानिक लाके तंत्र के केंद्र में पंथनिरपेक्षता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, संघवाद, स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्थाएँ बहुदलीय प्रणाली और शक्तियों के पृथक्करण, आदि सार्वभौमिक मूल्य के रूप में अभिव्यक्त हैं। इस शोध आलेख में संविधानिक भारतीय लाके तंत्र के इन्हीं कुछ मूल्यों के अवश्यम्भाविता का परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य संबद्ध आयाम जैसे संविधान का देश के सर्वोपरि विधि संहिता एवं इससे जनित संविधानवाद की बहस, संविधानवाद के वैकल्पिक प्रारूप की संभाव्यता का विमर्श , आदि का इस शोध आलेख में विश्लेषण किया गया है।
Authors :
प्रोफेसर अभय प्रसाद सिंह : (पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)
डॉ. कृष्ण मुरारी : (शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)
डॉ. रूपक कुमार : (शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.1
Price: 251
भारतीय लोकतंत्रा, संरचनात्मक असमानता और मुफ्तखोरी संस्कृति
By: पंकज लखेरा
Page No : 17-37
Abstract
16 जुलाई 2022 को अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्तखोरी संस्कृति या उनके ही शब्दों में कहें तो रेवाड़ी संस्कृति की आलाचे ना की और कहा कि यह देश के विकास के लिए खतरनाक होगी। वह बुन्देलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर जनता को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद इस तरह के गलत व्यवहार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। अदालत ने मामले को देखने के लिए सभी हितधारको को शामिल करते हुए एक विशेष समिति बनाने का फैसला किया, लेकिन बाद में मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भजे दिया। अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों द्वारा भरे जाने के लिए एक मानक पोरफार्मा जारी किया, जिसमें बताया गया कि वे अपने चुनावी वादों को कैसे पूरा करेंगे। हालाँकि, कई विपक्षी दलों ने इस आधार पर चुनाव आयोग के कदम की आलाचे ना की कि यह उनके लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसी ही घटना 2013 में हुई थी जब सुब्रमण्यम बनाम तमिल नाडु मामले में सुप्रीम कार्टे ने कहा था कि हालांकि मुफ्त वितरण को भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पार्टियों को अपने वादों के पीछे का तर्क बताना होगा और उन्हें वही वादे करने का आदेश दिया जिन्हें पूरा किया जा सके। लेकिन, इस बार यह मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया। इसने आवश्यक कल्याणकारी सेवाओं और मुफ्त वस्तुओ के रूप में सार्वजनिक धन की बर्बादी के बीच अंतर पर एक नई बहस को जन्म दिया। (साहू, घोष, चैरसिया, 2022) हमारे विचार में, हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उठाई गई यह बहस केवल सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयागे तक सीमित नहीं है। यह हमारे समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के माध्यम से लाके तंत्र को मजबूत करने के बारे में एक प्रासंगिक सवाल भी उठाता है। समय का सवाल यह है कि क्या केवल मुफ्त वस्तुओं के वितरण से इन वर्गों को सार्थक तरीके से मदद मिलेगी या हमारे समाज से संरचनात्मक असमानताओं को कम करके इन वर्गों का सशक्तिकरण संभव है? क्या ये मुफ्त उपहार हमारे लाके तंत्र को मजबूत करते हैं यालंबे समय में इसे कमजोर कर देंगे ?
Author :
पकंज लखेरा : सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, स्वामी श्रदानन्द काॅलेज दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.2
Price: 251
भारतीय कानून का व्याख्यात्मक अध्ययन एवं अवलोकन
By: चन्दन कुमार
Page No : 38-51
Abstract
इस आलेख में कानून क्या है? प्राचीन काल से लेकर अब तक के कानून के निर्माण एवं व्याख्याऔ पर चर्चा की गई है। काननू शब्द से अभिप्राय किसी देश या राज्य का अधिकारिक नियम से है जो दर्शाता है कि लोग क्या करे क्या न करे? इस संदर्भ में पशिचम और पूर्व के कानून की अवधारणाओं एवं व्याख्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इस लेख का मुख्य प्रश्न यह है कि भारत के संदर्भ में काननू का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक क्या स्वरूप रहा है और कैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थि क परिवर्तन का कानून के निर्माण एवं स्वरूप पर प्रभाव पड़ा है। प्राचीन काल की परम्परा और प्रथा अब नियम कानून के रूप में परिवर्तित होते जा रहे है। एवं इसकी व्याख्या में न्यायपालिका और न्यायाधीशो की भूि मका अहम हा गई है।
Author :
चन्दन कुमार : सहायक प्राध्यापक, दयाल सिंह संध्या कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.3
Price: 251
प्रधानमन्त्राी नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय संघवाद का परिद्रिश्य
By: पंकज कुमार सिंह , विजय शकंर चौधरी
Page No : 52-70
Abstract
भारतीय संघीय संरचना विश्व का एक विशिष्ट संघीय प्रतिरूप है। भारतीय संविधान में यद्यपि शाब्दिक तौर पर भारतीय गणराज्य को संघीय घाेि षत नहीं किया गया है तथापि राज्य को पर्याप्त संवैधानिक शक्तियाँ दी गइ र्हैं। संविधान के शब्दों की तुलना में भारतीय राजनीति की गतिशीलता ने भारतीय संघीय प्रणाली के कार्यकरण को वास्तव में निर्धारित एवं निरूपित किया है। एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली के दौर में जहाँ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल दिखाई देती है वही गठबंधन सरकारों के दौर में राज्यों के पक्ष में शक्तियों का संतुलन अपेक्षाकृत ज्यादा दृष्टिगत होता है। इस अध्ययन में यह विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है कि 30 वर्षों की गठबंधन राजनीति के बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्त्रव में एक दल की बहुमत प्राप्त सरकार आई हालाँकि इसे अन्य दलों का समर्थन प्राप्त था, इस एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली ने कैसे भारतीय संघीय संरचना एवं कार्यकरण को परिवर्तित किया है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कैसे और किस रूप में प्रभावित किया है ?
Authors :
डॉ. पंकज कुमार सिंह : सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)।
विजय शकंर चौधरी : शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.4
Price: 251
संसदीय लोकतंत्रा एवं विपक्ष : एक सैद्धांतिक उपागम
By: जया ओझा
Page No : 71-86
Abstract
समकालीन समय में संसद एक बहुआयामी संस्था के रूप में परिलक्षित होती है। केवल भारत में ही नहीं, अपितु संसदीय राजनीतिक व्यवस्था वाले अन्य देशो में भी यही स्थिति है। संसद के बहुत से कृत्य हैं, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना तथा देश के लिए सरकार का गठन करना है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष के अस्तित्व का अत्यंत महत्व है तथा यह स्वयं लोकतंत्र का सर्वाधिक विशिष्ट गुण है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत वाद, विमर्श तथा विमति की व्यवस्था अंतर्निहित होती है, जिसमें संवाद के लिए निरंतर अवसर एवं अनुकूलता बनी रहती हैं । एक गाँव की पंचायत से लेकर संसद तक सभी संस्थाएँ संवाद तथा विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होती है।अतएव संसदीय लाके तंत्र में एक स्थिर तथा सामथ्र्यशील विरोधी पक्ष उतना ही आवश्यक है, जितनी कि एक स्थिर सरकार। विपक्ष के द्वारा ही संसदीय लोकतंत्र में विचार-विमर्श, वाद, विवाद तथा संवाद संभव होता है। यद्यपि यह देखा गया है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दलीय प्रणाली व्याप्त हो परन्तु वहाँ विपक्ष सदैव मह्त्वपूर्व रहा है। ए॰ एल॰ लावेल के अनुसार “किसी भी दलीय प्रणाली की सफलता विपक्ष की वैधानिक मान्यता पर आधारित होती है”।प्रस्तुत आलेख संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की उत्पत्ति, उपस्थिति एवं उसकी उपादेयता के सैद्धांतक दृष्टिकोढ़ पर आधारित है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न दलीय प्रणालियों में भी विपक्ष के विविध स्वरूपों का विश्लेषण प्रसतुत करता है।
Author :
जया ओझा : पीएचडी शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.5
Price: 251
वन संसाधन, श्रेणीकरण और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी)
By: कमल नयन चौबे
Page No : 87-103
Abstract
श्रेणीकरण या कैटेगराइजेशन आधुनिक समय की महत्त्वपूर्ण परिघटना है। भारत में भी जनगणना के साथ जनसंख्या को विभिन्न श्रेणियों में बाँटने की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित रूप से आरंभ हुई। अमूमन यह माना जाता है कि श्रेणीकरण से राज्य को विभिन्न समूहों के बारे में कल्याणकारी नीतियाँ बनाने में आसानी होती है। बहुत से समूह खुद को गाले बंद करने और संसाधनों पर अपना हक जताने के लिए इन श्रेणियों का उपयोग करते रहे हैं। लेकिन यह भी माना जाता है कि जनसंख्या का श्रेणीकरण राज्य को विभिन्न समूहों का नियंत्रण करने में सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तुत आलेख भारत के संबसे वंचित समूहों में से एक पीवीटीजी (पार्टिकुलरली वलनरबे ल ट्राइबल ग्रुप्स या विशेष रूप से कमजारे जनजाति समूह) समूह की संरचना तथा इसके अंतर्गत आने वाली जनजातियों के जीविका और पहचान की सुरक्षा के लिए जद्दोजहद और इस संदर्भ में राज्य की भूमिका की पड़ताल करता है। डोंगरिया कोंध आदिवासियों के नियमगिरी संघर्ष के वृतातं के माध्यम से इस आलेख में इन समूहों के संघर्ष में कानून, नागरिक समाज और राज्य की भूमिका की पड़ताल की गयी है। आलेख यह तर्क देता है कि पीवीटीजी समूहों की भलाई के लिए बहुस्तरीय काम करने की आवश्यकता है, किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीविका और सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने की उनकी स्वायत्तता को मान्यता दी जाए, और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
Author :
कमल नयन चौबे : लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह काॅलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.6
Price: 251
स्थानिक राजनय, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं लोकप्रशासन
By: मीना रानी
Page No : 104-115
Abstract
राजनय या कूटनीति का स्थानीयकरण कोई नई राजनीतिक अवधारणा नहीं है। इसे पैराडिप्लोमेसी अथवा स्थानिक राजनय कहा जाता है। स्टीफन वोल्फ ने पैराडिप्लोमेसी को ‘उप-राज्य संस्थाओं की उनके महानगरीय राज्य से स्वतंत्र विदेश नीति में उनकी भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उनके अपने स्वयं के अंतरराष्ट्रीय हितो की खोज में उनकी विदेश नीति क्षमता‘ के रूप में वर्णित किया है। वोल्फ के लेखन में उप-राज्य संस्थाओं की उभरती नीति क्षमता के रूप में पैराडिप्लामे ेसी का आनंद संधो के राज्यों (या प्रांतों और क्षेत्रों) और स्वायत्त इकाई दोनों द्वारा किया जाता है। दुनिया के अलग-अलग देशों में कूटनीति का यह स्वरूप पिछले दो-तीन दशक में अधिक प्रचलन में आया है। एक लोकतांत्रिक संघीय प्रणाली वाले राष्ट्र के भीतर स्थानीय सरकारों की सक्रियता एवं आर्थिक बदलावों ने कूटनीति के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। व्यापार एवं निवेश से सम्बंधित आर्थिक कूटनीति में अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि चीन एवं रूस जैसे अधिनायकवादी देशो में स्थानिक कूटनीति लोकप्रिय हो चुकी है। इस आलेख के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया हैं कि भारत में भी र्कइ राज्य सरकारों ने पैराडिप्लोमेसी के माध्यम से देश की विदेश नीति को प्रभावित करने के साथ-साथ अपने लिए आर्थि क अवसरों में वृद्धि की है । स्थानिक राजनय से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को गति मिलती है जिसका प्रभाव लाके प्रशासन की पद्धतियों पर पड़ना स्वाभाविक है।
Author :
मीना रानी : सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.7
Price: 251
By: बलदेव सिंह नेगी
Page No : 116-131
Abstract
भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) 2021 के अनुसार 25.01 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीब है। दूसरी ओर भारत दूनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो 2026 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पुरे करेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर, 2022 में शहरी बेराजे गारी दर 7.2 प्रतिशत थी, जो ग्रामीण से अधिक है। बेरोजगारी या अल्प-रोजगार, शहरी क्षेत्रों में काम की आकस्मिक और रुक-रुक कर होने वाली प्रकृति ऋणग्रस्तता का कारण बनती है, जो बदले में गरीबी के संकट को मजबूत करती है। ये संकट काेि वड जैसी राष्ट्रीय आपदा के दौरान अधिक भयानक हो जाते हैं जो शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रभावित करता है और कभी-कभी विपरीत प्रवासन का परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में राज्य प्रायाेि जत नौकरी की गारंटी ग्रामीण या शहरी किसी भी इलाके के कमजोर श्रमिको के लिए आखिरी उम्मीद बन जाती है। कोविड-19 महामारी केदौरान मजदूरो के सामने रोजी -रोटी की समस्या आई और कुछ राज्यों ने समाधान के तौर पर अर्बन जॉब गारंटी की पहल की थी। वर्त मान शोध पत्र में शहरी गरीबों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजनाएँ बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारो की पहलों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए विभिन्न स्तोत्रों की सहारा लिया गया है जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की सालाना रिपोर्ट और ऑनलाइन डेटा, विभिन्न संस्थानों के शोध अध्ययन और समाचार पत्रों की रिपार्टे शामिल हैं।
Author :
बलदेव सिंह नेगी : परियोजना अधिकारी एवं संकाय सदस्य, ग्रामीण विकास, अंतःविषय अध्ययन विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल शिमला-171005.
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.8
Price: 251
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के सापेक्ष भारत में विलंबित न्याय और मानवाधिकार की समीक्षा
By: निशांत यादव
Page No : 132-147
Abstract
किसी भी समाज में शांति, सुरक्षा एवं सह-अस्तित्व बनाये रखने के लिए न्याय व्यवस्था का द्रुतगामी होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है परन्तु यदि भारतीय सन्दर्भ में बात करें तो यहाँ न्याय तक पहुँच बहुत ही जटिल व श्रम साध्य कार्य है। भारत में यदि विचाराधीन कैदियों के परिप्रेक्ष्य में न्याय तक पहुँच या त्वरित न्याय की जाँच-पड़ताल की जाए तो यह दृष्टिगत होता है कि यहाँ स्थिति पहले से ही ऐसी रही है कि मामूली अपराध के लिए भी व्यक्तियों को न्यायालय के आदेश के इंतज़ार में लम्बी अवधि तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में रहना पड़ा है। जिन्हे जमानत मिली, उन्हें भी अदालत के सालां-े साल चक्कर काटने पड़े और जो लोग न्याय पाने के लिए अदालत की शरण लेते हैं उन्हें भी न्याय के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, यदि मुकदमे समय पर खत्म नहीं होते, तो व्यक्ति पर जो अन्याय हुआ है, वह अथाह है । इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022 के आँकडो से इस हालात को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। भारत की जेलों में बंद केवल 22 प्रतिशत लागे ही सजायाफ़्ता मुजरिम हैं, 77.10 प्रतिशत बंदी विचाराधीन हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022 ने यह दावा कर बताया कि साल 2010 के मुक़ाबले 2021 तक विचाराधीन बंदियों की संख्या 2.4 लाख से बढ़कर 4.3 लाख पहुँच चुकी है, यानी करीब दोगुनी हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और पुदुचेरी को छोड़कर हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विचाराधीन क़ैदी बढ़े। प्रस्तुत लेख विचाराधीन बंदियों की इस समस्या को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के सापेक्ष रखकर मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता है।
Author :
डॉ. निशातं यादव : राजा बलवतं सिंह महाविद्यालय, आगरा में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.9
Price: 251
बालिका शिक्षा और साइकिलः बिहार सरकार की ‘मुख्यमंत्राी बालिका साइकिल योजना’ के प्रभाव का विश्लेषण
By: निशांत कुमार
Page No : 148-162
Abstract
बिहार के पाचं जिलों में किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर यह शोध महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की भूमिका की जांच करता है। यद्यपि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना कई ऐसे कारको का ख्याल रखने में बेहद सफल रही है जो स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में बाधा थी, लेकिन इसकी कल्पना एवं कार्यान्वयन में कुछ कमियां भी हैं। शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि भविष्य में योजना को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है अन्यथा इस सुविचारित योजना की सफलता भविष्य में निरर्थक साबित होगी।
Author :
निशांत कुमार : सह प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.10
Price: 251
राजस्थान में ग्रामीण व शहरी प्रवास के कारणाो का जेंडर पर आधारित विश्लेषणात्मक अध्ययन
By: शिव कुमार मीणा
Page No : 163-174
Abstract
जब कोई व्यक्ति अपने जन्म या जन्म से भिन्न स्थान पर जनगणना में पंजीकृत होता है तो उसे प्रवासी माना जाता है। प्रवास अनेक कारणों से हो सकता है कुछ लोगो के लिए रोजगार के अवसरो की तलाश या अपने जीवन को बेहतर करने की इच्छा। जबकि, कुछ मजबूरी के चलते तो कुछ अन्य लोगों के लिए अपने निवास स्थान की परिस्थितियाँ प्रवास के लिए विवश कर देती हैं। वर्तमान युग में तीव्र आर्थि क विकास, संचार की सरलता व लोगों के बीच आसान सम्पर्क के कारण लोग अपने जीवन को बेहतर करने हेतु अवसरों की खाजे में आसानी से पलायन कर जाते है। प्रस्तुत लेख में जेण्डर के विशेष संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो से तथा राज्यों में होने वाले प्रवास के कारणो का अध्ययन किया गया है। इसके लिए 2011 की जनगणना के द्वितीयक आंकड़ां का अध्ययन किया गया है। विश्लेषण से ज्ञात हुआ की ग्रामीण व शहरी प्रवासियों के अनुपात में मह्त्वपूर्ण अंतर है। यही अंतर जेण्डर के संदर्भ में भी देखने को मिलता है।
Author :
शिव कुमार मीणा : पी.एच.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.11
Price: 251
भारत में भारतीय संविधान के तहत सुशासन और सतत् विकास
By: लक्ष्मी परेवा
Page No : 175-188
Abstract
हर देश की प्रगति उसके शासन के स्तर पर निभर्र करती है। एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें निवासियों की भलाई एक सर्वोच्च चिंता है, मजबतू नेतृत्व की आवश्यकता है। मानव इतिहास में विभिन्न बिंदुआं पर स्थापित सुशासन के सिद्धांतो के विरूद्ध मापे जाने पर सरकार की वैधता को संदेह में कहा जा सकता है। यह सुनिश्चित करने में संविधान एक महत्वपूर्ण कारक है कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों के अनुसार काम करती है, क्यूंकि यह अधिकांश आधुनिक सरकारों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। लेकिन किसी भी तरह का शासन तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि वह विकास को बढ़ावा देने के लिए समय की उभरती जरूरतों के अनुकूल न हो उसी हद तक, आधुनिक युग दुनिया को सतत विकास के एक नए मॉडल की ओर बढ़ता हुआ देखता है, जिसके लिए आव्यशकताओ को अपने पारंपरिक सिद्धांतों के अलावा सुशासन के रूप मं शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए नए मापदंडो के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा, 17 सतत विकास लक्ष्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया और 2030 तक पूरा किया जाना है। इन 17 लक्ष्यां में से लक्ष्य 16 द्वारा सतत विकास को प्राप्त करने में सुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो सुशासन के लिए संस्थानों और प्रक्रियाओं की स्थापना की मांग करता है। सतत् विकास की अवधारणा के उदय के कारण और स्पष्ट बदलाव के आलोक में, यह लेख यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या भारतीय संविधान सुशासन की खोज मं इन नए विचारो को संबोधित करने के लिए जगह देता है और यदि हां, तो क्या देश की शासन प्रणाली इस तरह के शासन की स्थापना के लिए आवश्यक मापदंडों को बनाए रखने में सफल रही है।
Author :
डाॅ लक्ष्मी परेवा : सहायक आचार्य, लोकप्रशसन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.12
Price: 251
भारत में सकारात्मक कार्यवाही और आरक्षण
By: अरविन्द कुमार यादव
Page No : 189-224
Abstract
भारत में कई दशकों से सकारात्मक कार्यवाही नीति के तहत समाज के उपेिक्षत वर्गो को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। सरकार ने उपेक्षित वर्गों के चहुँमुखी विकास के लिए सामाजिक न्याय के तहत अनेक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसमें उनके समावेशीकरण करने के लिए अनेक नीतिया प्रमुख हैं। भारतीय समाज के उपेि क्षतों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजारे वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि आरक्षित वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर किया जा सके। संविधान का यह लक्ष्योन्मुख प्रावधान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र में आरक्षित समुदायों के ऊपर आरक्षण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को विभिन्न तथ्यां एवं आंकड़ों की सहायता से समीक्षा की गई है।
Author :
अरविन्द कुमार यादव : एसोसिएट पा्र ेफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, डाॅ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.02.13
Price: 251
By: ..
Page No : 225-229
Jul- to Sep-2023
By: ..
Page No : v
नागरिक-केंद्रित प्रशासनः समस्याएं और संभावनाएं
By: देवेन्द्र प्रताप तिवारी
Page No : 1-16
Abstract
संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे नागरिकों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, प्रशासनिक तंत्र संविधान की भावना के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा संविधान प्रशासन को नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की दिशा देता है। भारत में लोक नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन में सिविल सेवक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधकीय ढांचे की रीढ़ हैं। उनके कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका से लेकर स्वास्थ्य सेवा, भूमि से लेकर समुद्र तक और जीवन के लगभग हर क्षेत्र से जुड़े मामलों का प्रबंधन शामिल है। राज्य एवं सरकार के अधिकांश लक्ष्य इन अधिकारियों के प्रदर्शन से जुड़े हैं, जो विभिन्न क्षमताओं, विभिन्न पृष्ठभूमि और पर्यावरण से आते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में नागरिक-प्रशासन की चुनौतियों एवं संभावनाओं का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
Authors :
देवेन्द्र प्रताप तिवारी : सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, एस. एल. के. काॅलेज, सीतामढ़ी, (बी. आर. ए. बिहार, विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.1
Price: 251
By: संतोष कुमार सिंह
Page No : 17-40
Abstract
किसी भी राष्ट्र की प्रगति निश्चित रूप से उसके शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से लोकतंत्र ही वह उत्तम शासन व्यवस्था है जिसमें सभी के मानवाधिकार सुरक्षित रह सकते हैं । लोकतंत्र उन महत्वपूर्ण और बहुमूल्य उपहारों में से एक है जिसे सभ्यता ने मानव जाति को दिया है और जिसका सम्मान पूरी दुनिया की बहुसंख्यक आबादी करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की लोकप्रियता एवं महत्व का सार सूत्र है- मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आविर्भाव एवं स्थायित्व का संवाहक तत्व संविधान का आदर-सम्मान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, पंथनिरपेक्षता, विधि का शासन, शासन के अंगों के मध्य सामंजस्य, सत्ता का विकेन्द्रीकरण आदि तत्व मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की गतिविधियाँ हमेशा जनसरोकार की दिशा में क्रियाशील रहती हैं। इसमें सत्ता मशीनरी के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जाता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम की जा सके जिसमें एक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनादेश से सत्ता में बदलाव बहुत व्यवस्थित और सहज ढंग से हुआ है। भारत में लोकतंत्र का विकास सदियों का परिणाम है। भारत ने एक ऐसे लोकतंत्र का अपनाया है जिसमें मर्यादा, संयम और अनुशासन की झलक दिखाई देती है। दूसरी ओर आधुनिक भारत को ऐसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है, जिससे भारत की दशा और दिशा के सुनिश्चित प्रतिमान निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। इन चुनौतियों में शामिल हैंः सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी,अशिक्षा, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, आंतकवाद, नक्सलवाद आदि। यदि समय रहते भारत की अनेक चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता।
Auhors :
डाॅ संतोष कुमार सिंह : असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.2
Price: 251
संवैधानिक लोकतंत्र, लोक नीति एवं नागरिक समाजः समकालीन विमर्श
By: अभय प्रसाद सिंह’ एवं कृष्ण मुरारी
Page No : 41-56
Abstract:
संवैधानिक भारतीय लोकतंत्र ने विधिक और सार्वजनिक संस्थाओं की कुछ रचात्नामक और कुछ नियंत्रण-उन्मुखी औपनिवेशिक विरासत के साथ उत्तर-औपनिवेशिक गणतंत्र का सफर शुरू किया। संहिताबद्ध कानून, नौकरशाही और संख्या की राजनीति लोकतांत्रिक व् नीति प्रक्रियाओं की औपनिवेशिक विरासत के कुछ प्रतिगामी पहलू हैं जिसके परिणामस्वरूप आज तक भ्रष्टाचार एवं जातिगत और अन्य पहचान की राजनीति प्रचलन में है। हालाँकि, सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार की आधुनिक संस्थाओं ने भारत में परिवर्तनकारी लोकतांत्रिक फल्क्रम के रूप में काम किया है। आंदोलनों से उत्पन्न राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक नीति प्रक्रिया को सार्वजनिकता प्रदान की और धीरे-धीरे भारतीय लोकतंत्र को अधिक से अधिक प्रतिनिध्यात्मक और सहभागी बना दिया। सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलनों, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया, बाजार और शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे नागरिक समाज के घटक ने भी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को सृजनात्मक रूप से बदल दिया है और भारतीय लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बना दिया है। लोक कल्याण के निमित्त लोक सेवा प्रदायगी अभिकरणों एवं लोक नियामक संस्थाओं की महत्ती भूमिका ने भारतीय लोकतंत्र को वैश्विक लोकतान्त्रिक विश्व में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है । बहरहाल, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी चुनौतियाँ भारतीय लोकतंत्र में नीति विमर्श के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
Authors:
अभय प्रसाद सिंह: प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
कृष्ण मुरारी: असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.3
Price: 251
संवैधानिक लोकतंत्र और समकालीन समाज की चुनौतियाँ
By: कन्हैया लाल
Page No : 57-79
Abstract
भारत विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक-लोकतांत्रिक देश है जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, और संस्कृति के लोग साथ रहकर अनेकता में एकता का परिचय देते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य मे भारत अमृत महोत्सव मना रहा है जो भारत के संविधान की सफलता, परिपक्वता और भारतीय समाज मंे उभरते नये आयाम को प्रदर्शित करता है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास पर बल दिया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, लोकप्रभुसत्ता, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों व मूल्यों आदि पर विश्वास व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान को अपनाया जाना करोड़ों लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण पल था। के.एम. पानिकर के अनुसार, ‘‘संविधान लोगों को दिया गया दृढ़ वचन है कि कानून समाज को नए सिद्धांतों पर पुर्नस्थापित करेगा व नूतन व्यवस्था में लाएगा।’’ भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के अपने कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं - लोकप्रभुसत्ता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, राजनीतिक भागीदारी, वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी सरकार आदि।
भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने का सम्मान प्राप्त है, लेकिन इसके कुछ चुनौतियाँ भी हैं। वास्तव में भारतीय लोकतन्त्र केवल लोकतन्त्रीय सरकारें संगठित और संचालित करने में ही सफल हुआ है, इसे अपने सामाजिक-आर्थिक पहलूओं में अभी सफलता प्राप्त करनी है। इसमें जो प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं वे हैंः सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अलगाववाद और राजनीतिक हिंसा। ग़रीबी और बेकारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और लोगों को स्व-रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बिजली यातायात और संचार सुविधाओं आदि की व्यवस्था व्यापक और व्यवस्थित रूप में की जानी चाहिए।
Author:
कन्हैया लाल: सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एस. मेमोरियल महाविद्यालय, राँची,राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.4
Price: 251
भारत में लोक केन्द्रित प्रशासनः सिद्धान्त एवं व्यवहार
By: अखिलेश कुमार जायसवाल
Page No : 80-96
Abstract:
21वीं सदी में हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जिसे प्रशासकीय राज्य भी कहा जाता है, जो मानव जीवन के हर पहलू को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। प्रशासकीय राज्य को लोककल्याणकारी बनाने हेतु शासन-प्रशासन के जन केन्द्रित होकर कार्य करने पर बल दिया जाता है और इसी कारण लोक केन्द्रित प्रशासन की अवधारणा ने जन्म लिया जिसमें जन कल्याण को प्रशासन के केन्द्र में रखा जाता है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था लोक केन्द्रित होने की दिशा में निरन्तर अग्रसर है और भारतीय प्रशासन को लोक केन्द्रित बनाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे- संवैधानिक प्रावधान, कानून-निर्माण द्वारा लोक संस्थाओं का गठन- लोक शिकायत निदेशालय, नागरिक चार्टर्स, लोकपाल व लोकायुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सूचना का अधिकार, विभिन्न आयोग एवं न्यायाधिकरण एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश व योजनाएँ। इन सबके बावजूद अभी भी भारत की प्रशासनिक तंत्र में अनेक व्यवस्थागत खामियां व्याप्त हैं, जैसे-भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, लालफीताशाही, आमजन के प्रति लोक सेवकों का उदासीन रवैया, प्रशासन में राजनैतिक हस्तक्षेप आदि। लेकिन तकनीकी क्रान्ति व आमजन की जागरूकता ने धीरे-धीरे प्रशासन को लोक केन्द्रित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है।
Author:
अखिलेश कुमार जायसवाल: असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हिन्दू पी0 जी0 काॅलेज, जमानियाँ, गाजीपुर, उ0 प्र0-233131,
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.5
Price: 251
लोक केन्द्रित प्रशासन के वर्तमान अस्थायी प्रयास और स्थायी तन्त्र की संभावनाएँ
By: जोरावर सिंह राणावत
Page No : 97-114
Abstract
लोक प्रशासन शब्द का अर्थ स्वयं में ही लोक केन्द्रित प्रशासन है तथा जिसका अर्थ जनता के लिए प्रशासन से लगाया जा सकता है। प्रशासन के प्रमुख लक्षणों में से एक विकेन्द्रीकरण है जो शासन का अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचना सुनिश्चित करता है। प्रशासन को पारदर्शी, प्रभावशाली, कार्यकुशल, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य जनता की इस तक पहुँच कोे सुगम बनाना तथा सेवा प्रदायगी और शिकायत निवारण को त्वरित बनाना है। इसे ही सुशासन एवं कुशल प्रशासन कहा जाता है और इसे ही रामराज की संज्ञा भी दी जाती है। प्रत्येक सरकार स्वयं को ऐसा बनाने और जनता तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कई प्रयास करती हैं। वर्तमान में भी विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा प्रशासन आपके द्वार, शासन आपके संग जैसे अस्थायी प्रयास के द्वारा जनता की शिकायतों का निवारण किया जाता है और जनता के लिए सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जाती है। प्रस्तुत लेख में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे ऐसे कार्यक्रमों का अनुभवमूलक मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए इनकी कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है।
प्रस्तुत लेख में यादृच्छिक निदर्शन विधि द्वारा 100 व्यक्तियों का निदर्श के रूप में चुनाव किया गया है जिसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनसे प्राप्त अनुभवमूलक प्रतिक्रियाओं द्वारा लोक केन्द्रित प्रशासन के लिए सरकार द्वारा किये गये अस्थायी प्रयासों का विश्लेषण करते हुए स्थानीय स्तर पर एक स्थायी तन्त्र के विकास का माॅडल प्रस्तुत किया है जिसमें लोक केन्द्रित शिकायत निवारण एवं सेवा प्रदाता केन्द्र की स्थापना का प्रावधान किया है। यह केन्द्र स्थानीय स्तर की समस्त सेवाओं तथा शिकायतों के निवारण के लिए ’सिंगल विण्डो’ की तरह विकसित किया जा सकता है। लेख में इस केन्द्र की स्थापना में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करते हुए उनके निवारण के लिए समाधान भी प्रस्तुत किये गए हैं।
Author
जोरावर सिंह राणावत: सहायक आचार्य एवं सहायक अधिष्ठाता, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, कला एवं मानविकी संकाय, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.6
Price: 251
By: राकेश कुमार
Page No : 115-127
Abstract:
डाॅ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का महिलाओं के संदर्भ में मानना था की “मैं समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ। शादी करने वाली हर लड़की अपने पति के साथ- साथ खड़ी हो, अपने बराबर होने का दावा करे और उनकी दासी बनने से इंकार करे मुझे यकीन है कि यदि आप इस सलाह का पालन करते हैं, तो आप सम्मान वह गौरव लाएगें” (सिंगारिया, 2014)। भारत की राजनीति में महिलाओं की हालिया भागीदारी से कुछ बिंदु स्पष्ट हैं पहला, लगातार पिछले कुछ वर्षों से महिला मतदान प्रतिशत में हो रही बढ़ोतरी 2019 के लोकसभा चुनाव में अब तक के शीर्ष स्तर पर पहुच गई है दूसरा, राजनैतिक दलों के चुनाव प्रचार से लेकर सरकारों की विभिन्न योजनाओं तक का निर्माण महिलाओं को केंद्र में रख कर किया जा रहा है। महिलाओं का मतदान प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन मुख्य प्रश्न यह है की क्या महिला मतदाता किसी तरह का राजनीतिक बदलाव करने में सक्षम है? इस अध्ययन में महिलाओं के मतदान व्यवहार पर भी चर्चा की गई है।
इस अध्ययन के लिए द्वितीय स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है। तथा वर्तमान में उभरते मतदान प्रतिरूप पर चर्चा की गई है। संसद वह राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी जनसख्याँ के अनुपात में बहुत कम रहा है इसके बावजूद भी संसद महिला आरक्षण बिल को स्वीकृति नही दे पाई है। राजनैतिक दलों ने अपने दल के भीतर महिला विंग का निर्माण तो किया है परन्तु चुनावों में महिलाओं को टिकट देने में अभी भी दल बहुत पीछे है। इसके बावजूद भारत की चुनावी राजनीति मे महिलाओं का मतदाता के रूप मे उभार देखने को मिला है जोकि चुनाव के परिणामों को भी प्रभावित करने मे सक्षम है। इस अध्ययन में महिलाओं की चुनावी भागीदारी को एतिहासिक दृष्टि से दर्शया गया है तथा उनकी बढती भूमिका के कारण भारतीय राजनीति में हो रहे परिवर्तनों पर चर्चा की गई है।
Author
राकेश कुमार: शोधार्थी-राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय) लखनऊ।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.7
Price: 251
ई-गवर्नेंस तथा जिला प्रशासन में नवाचार
By: धनंजय शर्मा
Page No : 128-141
Abstract
जब किसी भी राज्य के प्रशासन को आसानी व सुगमता से चलाने के लिए राज्यों को संभागों व संभागों को जिलों में विभक्त किया गया है। जिला प्रशासन राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना है, जो राज्य के सचिवालय तथा तहसीलों के मध्य समन्वयक कड़ी भी भूमिका निभाता है। जिला प्रशासन जिले में सरकार के समस्त कार्य करता है। इसी कारण किसी भी राज्य की ‘सुरक्षा‘ एवं ‘विकास‘ जिला प्रशासन की परिधि में आते हैं। ई-गवर्नेंस सुशासन का महत्वपूर्ण घटक है। भारत में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन लाने की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके। ई-गवर्नेंस का माॅडल अपनी जगह पर स्थापित करने के प्रयास जारी है। सरकार तथा नागरिकों के बीच मौजूद दूरियाॅ भी कम हुई हैं। इंटरनेट, मोबाइल फोन और गाॅव-गाॅव, शहर-शहर में फैले सरकारी सेवा प्रदाताओं (कियोंस्क) के माध्यम से लोग पहले की तुलना में ज्यादा आसानी से सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जिससे प्रकियाएँ सरल हुई हैं तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। तथा ई-गवर्नेंस से संबधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की भी एक बड़ी भूमिका है।
Author:
धनंजय शर्मा: सहायक प्रध्यापक (समाजशास्त्र), रानी धर्म कुॅंवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला-खानपुर, हरिद्वार, (उत्तराखण्ड )
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.8
Price: 251
जिला स्तर का प्रशासन और उपयोगी नवाचार
By: पूजा गुप्ता एवं निलांजना जैन
Page No : 142-150
Abstract:
यह लेख भारतीय प्रशासनिक जिलों की ओर नवाचार के रुझान की गंभीर रूप से विश्लेषण करता है। यह 21वीं सदी के नवाचार जिले को प्रमुखता से समझने का एक प्रयास है। नवाचार जिलों का प्रशासन एक विशेष ज्ञान व रुझान पर आधारित होता है। जो आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की रणनीति तय करने में सहयोग करते हैं तथा प्रक्रिया और उत्पाद के लिए आवश्यक माने जाने वाले अभिनेताओं और संस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचों पर ध्यान केंद्रित करते हैं । नवाचार का प्रमुख लक्ष्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। यह लेख मुख्यता भारतीय प्रशासनिक जिलों द्वारा बनाए जा रहे नवाचार के साधनों और योजनाओं का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा भारत जैसे वृहद विविधता पूर्ण देश में प्रशासनिक सुधार और विकास को बढ़ावा मिले। प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक जिलों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे उपयोगी नवाचार के वृहद अध्ययन को प्रस्तुत करना है।
Author:
पूजा गुप्ता: आर्य कन्या डिग्री कालेज, संबद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
निलांजना जैन: प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, संबद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.9
Price: 251
ग्रामीण लोक केंद्रित व्यवस्था हेतु पुरा-परियोजना की संकल्पनाः आशा एवं निराशा
By: सुशांत यादव
Page No : 151-161
Abstract:
कोरोना महामारी जैसे वैश्विक संकट से आज पूरा विश्व भयभीत है और इसके दुष्परिणामों को विश्व के तमाम देशों के साथ भारत भी झेल रहा है। महामारी के इस माहौल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली संख्या गरीब व्यक्तियों की हैं। जिनका अधिसंख्य मूल निवास भारत के गाँवों में हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए.पी.जे अब्दुल कलाम का मानना था कि गाँवों में बसे व्यक्तियों को समाहित किए बग़ैर हम भारत की पूर्ण तस्वीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतः विकास से संबंधित किसी भी नीति का निर्माण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि, वह ग्रामीण भारत की आवश्यकता को किस हद तक पूर्ण कर सकता है। अगर वह नीति इन अधिसंख्य भारतीयों की आवश्यकता को स्वयं में समाहित नहीं करती तो नीति निर्माण संस्थानों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गांवों का सामाजिक-राजनीतिक जीवन दर्शन महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर एवं स्वायत्त गांवों की संकल्पना से लेकर ए.पी.जे अब्दुल कलाम की पुरा (प्रोविज़न आफ अर्बन एमेनीटिज़ टू रूरल एरियाज.) परियोजना तक भारत के ग्रामीण समाज के सामाजिक राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वैसे तो आत्मनिर्भरता की अवधारणा एवं पुरा परियोजना की संकल्पना दोनों ही विशुद्ध अर्थशास्त्रीय संकल्पनाएँ हैं, परन्तु समाज का अर्थशास्त्र, समाज एवं समाज की राजनीति दोनों को अपरिहार्य रूप से प्रभावित करती है। इसी अर्थशास्त्र के कारण गावों का समाज एवं इसकी राजनीति हमेशा से अद्वितीय एवं अनोखा चित्र प्रस्तुत करते आये हैं। उपर्युक्त आलेख में गाँव-शहर के इसी सम्बंधों पर कलाम के पुरा परियोजना की अवधारणा से समबंधित विचारों और पहलुओं का मूल्याँकन प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया गया है।|
Author
सुशांत यादव: कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मवाना (मेरठ, उ.प्र.)
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.10
Price: 251
लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में किशोर न्याय प्रशासन
By: सुमिता मुदगल
Page No : 162-172
Abstract
भारतीय शासन व्यवस्था में राज्य मनुष्य की उस समुदाय से संबंधित संकल्पना है जो एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर परस्पर संगठित होकर अपनी एक संप्रभु सरकार स्थापित करती है। मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को विभिन्न विचारधाराओं में से किसी ने राज्य को एक दमनकारी संस्था के रूप में परिभाषित किया तो किसी ने राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। प्राचीन भारत की रामराज्य धारणा का विकसित रूप वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में दृष्टिगत होता है। नैतिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसे राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का चहुँमुखी विकास और कल्याण करना है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में चिन्हित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा समाज कल्याण प्रशासन की महत्वता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सन् 1985 में कल्याण मंत्रालय स्थापित किया जिसे 1998 में परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के रूप में पुर्नस्थापित किया गया। सरकार द्वारा कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधिक प्रयास भी किए गए जिसमें से एक प्रयास किशोर न्याय (बालकों की सुरक्षा एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 के रूप में परिलक्षित होता है जो बालकांे की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए स्थापित विभिन्न संस्थाओं के रूप में समाज में किशोर न्याय प्रशासन की वकालत करता है। उक्त अधिनियम में वर्णित विभिन्न सिद्धांत तथा कानूनी प्रावधान बालकों की देखरेख एवं सुरक्षा को लेकर राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका को उजागर करते हैं।
Author
सुमिता मुदगल: शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.03.11
Price: 251
By: सुमिता मुदगल
Page No : 173-175
Price: 251
Oct- to Dec-2023
By: ..
Page No : v
एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, राजनेता, सांसद एवं प्रधानमंत्री
By: श्रीप्रकाश सिंह , धारासिंह कुशवाहा
Page No : 1-14
Abstract
स्वाधीनता पश्चात काल में, भारतीय लोकतंत्र की दशा एवं दिशा के निर्धारण में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। एक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राजनेता, सांसद, विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कार्यचालन के सन्दर्भ में अपना विशेष योगदान दिया है। वास्तव में, एक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान बहुआयामी रहा है।
स्वाधीन भारत के राजनीतिक मानचित्र पर, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक राजनेता की भूमिका में करीब पाँच दशक से अधिक का समय बिताया। अक्सर उन्हें आपसी सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित राजनीतिक नेतृत्व शैली संबंधी विशेषताओं के लिए याद किया जाता रहा है। अपनी विलक्षण वाक्पटुता एंव तर्कसंगत टीका-टिप्पणी की योग्यता के चलते, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय संसदीय संस्थाओं के सुसंगत संचालन में वृहद, विशेष एवं उल्लेखनीय योगदान दिया है। व्यावहारिक राजनीति में भी, पहले भारतीय जनसंघ तथा बाद में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी राजनीतिक यात्रा के चरम पर, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय लोकतंत्र के ‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वकर्ता’ की भूमिका भी निभाई और तीन बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला।
Authors :
श्रीप्रकाश सिंह: आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
धारासिंह कुशवाहा: शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.1
Price: 251
भारत मे नौकरशाही अनिर्णय और सुधारः नौकरशाही प्रदर्शन और मिशन कर्मयोगी की आवश्यकता का विश्लेषण
By: प्रवीण कुमार झा , संगीता
Page No : 15-25
Abstract
नौकरशाही संस्था प्राचीन काल से अस्तित्व में है और संस्था को हमेशा ऐसे कर्तव्य सौंपे गए हैं जिनके लिए बुद्धि, साहस की आवश्यकता होती है और साथ ही यह अधिकारियों को बहुत उच्च स्तर की शक्ति प्रदान करती है। भारतीय नौकरशाही को भी ऐसी शक्ति, जिम्मेदारी और निर्णय लेने की शक्ति सौंपी गई है। लेकिन इस संस्था की अक्सर भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण, लालफीताशाही और नौकरशाही के आरोपों के साथ आलोचना की जाती रही है। हालाँकि यह संस्था राष्ट्र की क्षमता निर्माण के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन यह नेताओं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में काफी हद तक विफल रही और जल्द ही यह संस्था समय की माँगों को पूरा करने में कम कुशल और कम प्रभावी हो गई। इस लेख का उद्देश्य भारतीय नौकरशाही में निहित समस्याओं और मिशन कर्मयोगी द्वारा सुझाए गए सुधारों का अध्ययन करना है।
Authors :
प्रवीण कुमार झा: प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
संगीता : प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह काॅलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.2
Price: 251
वैश्वीकरण 4.0 की दिशा में एक समावेशी दृष्टिकोण पर काम करनाः लैंगिक चिंताओं के महत्व पर एक केस स्टडी
By: आमना मिर्जा , अक्षिता नागपाल
Page No : 26-35
Abstract
इस शोध पत्र का उद्देश्य लैंगिक असमानताओं और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाली आर्थिक उदारीकरण सम्बन्धी नीतियों का अवलोकन करना है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैश्वीकरण ने दुनिया में लैंगिक संबंधों को कैसे प्रभावित किया है। अध्ययन में वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को शामिल किया गया है। व्यापक आर्थिक नीतियों के परिणामों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहित विभिन्न अभिनेताओं द्वारा की गई पहल को शामिल किया गया है। यह शोध पत्र इस वैश्वीकृत
दुनिया में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर सिफारिशों का एक अध्ययन सामने रखता है। शोधपत्र कई खंडों में विभाजित है जो वैश्वीकरण के सभी पहलुओं, वर्षों में इसके परिवर्तन और महिलाओं के जीवन में हुए प्रभावों के बारे में चर्चा करता है।
Authors :
आमना मिर्जा : असिस्टेंट प्रोफेसर, एसपीएम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
अक्षिता नागपाल : डॉक्टरेट रिसर्च स्कॉलर, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.3
Price: 251
भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टताएंः एक शोध अन्वेषण
By: अभय प्रसाद सिंह , कृष्ण मुरारी
Page No : 36-53
Abstract
भारतीय लोकतंत्र की विरासत औपनिवेशिक अनुभव, स्वतंत्रता आन्दोलन में विकसित साझी दूर दृष्टि एवं जन नायकों के सृजनात्मक कल्पनाशीलता का एक विशिष्ट संविधानिक अभिव्यक्ति है। नागरिक, राजनीतिक दल, शासकीय निकाय, न्यायपालिका,एवं नागरिक समाज के घटकों ने विगत साढ़ेसात दशकों में एक विमर्शी एवं समावेशी लोकतंत्र स्थापित किया है। दुनिया के प्राचीनतम एवं समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भारतीय लोकतंत्र अपने विशिष्टताओं के कारण संविधानवाद की एक अलग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस शोध आलेख में भारतीय लोकतंत्र के विशिष्टता विमर्श के प्रमुख आयामों जैसे, सामाजिक एवं जेंडर न्याय, शासकीय
नियामक अभिकरण, राजनीतिक संस्कृति, सार्वभौमिक मताधिकार, मतदान व्यव्हार, आदि, का विद्वत विश्लेषण किया गया है।
Authors :
अभय प्रसाद सिंह : प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
कृष्ण मुरारी : असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.4
Price: 251
भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, बदलता स्वरूप एवं प्रभाव
By: सोनम
Page No : 54-65
Abstract
सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) बड़े और छोटे दोनों उद्यमों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जवाबदेही देता है। यह तब होता है जब कोई कंपनी न केवल अपने लाभ में वृद्धि के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर समाज की भलाई के लिए सकारात्मक और प्रभावी ढंग से योगदान देकर उपभोक्ता विश्वास स्थापित करने के लिए भी काम करना चुनती है। आजकल कई निजी औद्योगिक एवं व्यावसायिक निगम महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाएं चला रहे हैं, जो पूरी तरह से भारत में सीएसआर परियोजनाओं के तहत सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। 2013 अधिनियम के तहत इन जवाबदेहियों के
क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के मुख्य अधिकारी या मुख्य स्थिरता अधिकारी (सीएसओ) कहा जाता है। (जेएसडीएम, 2022) इस शोध आलेख में 2013 के नई कंपनी अधिनियम के लागू होने के बाद सीएसआर में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, दस शीर्ष कंपनियों के सीएसआर के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की प्राथमिकता का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
Author:
डा. सोनम : वाणिज्य विभाग, शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.5
Price: 251
समावेशी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः अवसर और चुनौतियाँ
By: पंकज लखेरा
Page No : 66-83
Abstract
शिक्षा व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने की प्रक्रिया है। वस्तुतः शिक्षा की यही अवधारणा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक सभी शिक्षा प्रणालियों में सदैव रही है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1966 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति, 2008 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की शिक्षा नीतियों को अपनाया। उपरोक्त सभी नीतियों में शिक्षा को अधिक से अधिक छात्र-हितैषी, रोजगारोन्मुखी, समावेशी, सुलभ और स्थानीय परिवेश के लिए उपयुक्त बनाने के सभी प्रयास किए गए। लेकिन फिर भी, इतने ईमानदार कदमों के बावजूद, शिक्षा की पूरी प्रणाली की अक्सर उबाऊ, बोझिल, गैर-समावेशी, गैर-सुलभ और गैर-रोजगार उन्मुख होने के लिए आलोचना की जाती है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए और शिक्षा को उत्कृष्ट स्तर का बनाने के लिए,वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद और लाखों व्यक्तियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। हितधारकों वर्तमान पेपर विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का विश्लेषण करना चाहता है। यह नीति समाज के इस विशेष वर्ग की कितनी मदद करने वाली है? इस नीति के सकारात्मक पहलू क्या हैं? जहाँ तक विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों का सवाल है, इस नीति में कुछ कमियाँ और चुनौतियाँ हैं?
Author:
पंकज लखेरा : एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.6
Price: 251
स्वतंत्रतापूर्व भारत में किसान आंदोलन: एक विश्लेषण
By: सीमा दास , कामना कुमारी
Page No : 84-93
Abstract
कृषि भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का आधार रही है। ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक काल में बदली हुई भूमि व्यवस्था व भू-राजस्व की नवीन पद्धतियों के कारण किसानों का शोषण सर्वाधिक हुआ। जमींदारों,साहूकारों, महाजनों आदि के शोषणकारी चरित्र ने किसानों की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया था। बढ़े हुए लगान, कर्ज व बेरोजगारी के दुष्चक्र ने किसानों की स्थिति को दयनीय कर दिया था। किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया, जिससे वो ऐसी स्थिति में पहुँच गए जो दास व्यवस्था जैसी थी। सरकार द्वारा मालगुजारी प्रत्यक्षतः वसूलने की भूमिका त्याग दी गई और इसके लिए नवीन रास्ते अपनाए गए जैसे लगान की बढ़ती दर, व्यापार के क्षेत्र में घुसपैठ, उपभोक्ता सामान पर बढ़े हुए कर तथा दिनों दिन बढ़ता कर्ज। जिससे जमींदारी प्रथा का विकास होता चला गया। भारत के आर्थिक-सामाजिक ढांचे के भीतर मौजूदा अंतर्विरोधों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अशान्ति बढ़ा दी। अतः किसानों ने अपने शोषण के विरूद्ध व अधिकारों की प्राप्ति के लिए विद्रोह किए। समयानुसार किसान आंदोलन की प्रकृति में परिवर्तन आया।
प्रस्तुत शोध पत्र का केंद्रबिन्दु स्वतंत्रता सेे पूर्व हुए महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हैं। जिनका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं उनके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्ययन में आवश्यकतानुसार द्वितीयक सामग्री-शोध पत्र, पुस्तक, लेख, शोध प्रबंध आदि का प्रयोग किया गया है।
Authors :
डा. सीमा दास : सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, महिला विश्वविद्यालय, बी.एच.यू. उत्तर प्रदेश।
कामना कुमारी: शोधकर्ता, राजनीति शास्त्र विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.7
Price: 251
ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से संबंधित नीतियाँः पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में अध्ययन
By: पांचाली मजूमदार
Page No : 94-102
Abstract
स्मारक संरचनाएं या इमारतें हैं जो अपनी संस्कृति और स्थापत्य विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भारतीय इतिहास के लंबे समय तक चलने वाली और लोकप्रिय प्रतीक हैं क्योंकि वे उनके बारे में राजनीतिक और ऐतिहासिक जानकारी दर्शाते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है, इसलिए उन्हें बहाल करने की आवश्यकता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, जबकि भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरातत्व सर्वेक्षण और पश्चिम बंगाल हेरिटेज कमीशन जैसे राज्य स्तर के निदेशालय रखरखाव और संरक्षण में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक स्मारक उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सबसे उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। हालांकि, ऐसे कई स्मारकों की मरम्मत और पुनसर््थापन की आवश्यकता है। इस पत्र का उद्देश्य औपनिवेशिक युग से लेकर आज तक विरासत स्मारकों के संरक्षण के संबंध में ली गई नीतियों का विश्लेषण करना है, और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मामले पर केंद्रित है।
Author :
पांचाली मजूमदार : सह आचार्या, रामकृ ष्ण श्रद्धा मिशन, विवेकानंद विद्याभवन, कोलकाता
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.8
Price: 251
बिहार के खनिज संसाधनों का भौगोलिक सर्वेक्षण: बिहार के विकास के संदर्भ में नीति-निर्माण हेतु रोडमैप
By: शशि भूषण
Page No : 103-123
Abstract
झारखंड निर्माण के बाद आम धारणा बन गयी कि बिहार खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन प्रदेश रह गया है। जबकि भौगोलिक-भूवैज्ञानिक यथार्थ यह है कि यद्यपि लौह-अयस्क, ताम्र-अयस्क एवं बॉक्साइट सदृश अनेक प्रकार की खनिज संपदा के व्यापक भंडार झारखंड के हिस्से में चले तो गए, तथापि धात्विक (हेमेटाइट व मैग्नेटाइट सदृश लौह धातुएँ, ताँबा व सीसा जैसी अलौह धातुएँ, बॉक्साइट प्रभृती हल्की अलौह धातु व सोने के रूप में बहुमूल्य अलौह धातु), अधात्विक (अभ्रक, एसबेस्टस, गंधक, चूना-पत्थर, बेराइट, क्षारीय नमक, सोडियम नमक, पोटाश, विविध प्रकार की मृत्तिकाएँ साधारण मृत्तिका, चीनी मिट्टी, अग्निसह मृत्तिका, मुल्तानी मिट्टी व सुघत्य मिट्टी, भवन निर्माण के पत्थर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट-नीस, लैटेराइट, बालू-पत्थर, क्वाटर््जाइट व स्लेट, अलंकारी चट्टान, रोड मेटल, बहुमूल्य पत्थर व खनिज-जलस्रोत), आणविक (यूरेनियम, थोरियम, कोलम्बियम-टैन्टेलम, बेरिल व ग्रेफाइट) तथा अन्य प्रकार के खनिज संसाधनों (डोलोमाइट, फेल्सपार, सिलिका बालू, बालू-पत्थर, ट्रिपलाइट व काँच निर्माण के खनिज) का बिहार में उल्लेखनीय संचयन के साथ ही उनकी मौजूदगी की अतिरिक्त संभावनाएँ भी विद्यमान हैं। इस अध्ययन में बिहार के खनिज संसाधनों का गहन भौगोलिक सर्वेक्षण करते हुए नीति-निर्माण हेतु रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त सरकारी नीति-निर्माण व कुशल तकनीक का तार्किक अनुप्रयोग करके खनिज संसाधनों की उपलब्धता की पुष्टि करके उनका समुचित उत्खनन किया जाना समय की माँग है। इससे राज्य के औद्योगिक सह आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
Author :
शशि भूषण : वैज्ञानिक, पर्यावरण शोध एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.9
Price: 251
By: राकेश कुमार , सिद्धार्थ मुखर्जी
Page No : 124-145
Abstract
दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रही है। आजादी के बाद दिल्ली की जनसांख्यिकी में कई परिवर्तन आए हैं, अगस्त 1947 में लगभग पाँच लाख शरणार्थी दिल्ली आए थे (राज एवं सहगल, 1961)। दिल्ली की जनगणना के आंकड़ों में, 1941-51 के बीच, दिल्ली की जनसंख्या में 90 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी (राज एवं सहगल, 1961)। इसके पश्चात् मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों के तेजी से प्रवासन के परिणामस्वरूप दिल्ली के मतदाताओं की सामाजिक संरचना में बदलाव आया है। देश के अन्य राज्यों से भी लोग रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। हालाँकि यह प्रवासी मतदाता एक जातीय समूह से नहीं हैं और अपने मूल निवास स्थान, अपनी जाति और अपनी भाषा के संबंध में काफी विविधता रखते हैं। अलग-अलग राज्यों से आने वाले यह लोग दिल्ली में विभिन्न जातीय व धार्मिक समूहों का निर्माण करते हैं या अपने समूहों को संख्यात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह लोग अपने राज्य में जिस सामाजिक समूह से सम्बंधित होते हैं, दिल्ली में भी उसी समूह से प्रभावित होकर मतदान करते हैं? या दिल्ली में उनकें मतदान व्यवहार में कुछ अंतर होता है? क्या किसी समूह के मतदान व्यवहार में कोई स्थाई प्रतिरूप है? अथवा कोई समूह सामूहिक तौर पर किसी दल के प्रति आकर्षित रहा है? इस अध्ययन में दिल्ली के विभिन्न जातीय, धार्मिक समूहों के मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया है तथा उनके मतदान व्यवहार के प्रतिरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
Authors :
राकेश कुमार : शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
सिद्धार्थ मुखर्जी : सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.10
Price: 251
दफन होती जलनिधियाँः राजस्थान की जल-संस्कृति, समाज और विकासात्मक राज्य के संदर्भ में एक अध्ययन
By: रेखा कुमारी
Page No : 146-156
Abstract
जल वह बहुमूल्य संपत्ति हैं जिस पर संपूर्ण मानव सभ्यता का भूत, भविष्य व वर्तमान निर्भर करता है। यही कारण है कि विश्व में जितनी भी सभ्यताओं व संस्कृतियों का विकास हुआ वह मुख्यतः जल स्त्रोतों के आस पास ही हुआ। पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति के समय से ही मानव व प्रकृति के बीच एक प्रकार का रहस्य रहा है। परंतु आधुनिकता व पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप जिस प्रकार की तार्किकता व मानव बुद्धि का विकास हुआ उसने मानव व प्रकृति के बीच विद्यमान इस रहस्य को उद्घाटित करते हुए मानव मात्र को प्रकृति का दोहनकर्ता बना दिया है और आज स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि मानव बुद्धि द्वारा निर्मित यही ज्ञान, आज उसी के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न करने लगा है।1 इसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में हमारा यह लेख विशेष रूप से राजस्थान में जल संकट की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए, विकासात्मक राज्य व नागरिक समाज के बीच के अंतरसंबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता इसके अतिरिक्त जल प्रबंधन व संरक्षण के संबंध में सदियों से लगे समाज की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए, नागरिक समाज के संबंध में विद्यमान एकल समझ व विचार को पुनः परिभाषित कर नागरिक समाज की एक संदर्भ आधारित समझ प्रस्तुत करने की दिशा में एक प्रयास है।
Author :
रेखा कुमारी : पीएचडी शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
DOI : https://doi.org/10.32381/LP.2023.15.04.11
Price: 251
By: ..
Page No : 157-165
Price: 251
By: ..
Page No : 166-171
Price: 251
Instruction to the Author
• आलेख में सामग्री को इस क्रम में व्यवस्थित करेंः आलेख के शीर्षक, लेखकों के नाम, पते और ई-मेल, लेखकों का परिचय, सार संक्षेप, (abstract) संकेत शब्द, परिचर्चा, निष्कर्ष/सारांश, आभार (यदि आवश्यक हो तो) और संदर्भ सूची ।
• सारसंक्षेपः सारसंक्षेप (abstract) में लगभग 100-150 शब्द होने चाहिए, तथा इसमें आलेख के मुख्य तर्को का संक्षिप्त ब्यौरा हो। साथ ही 4-6 मुख्य शब्द (Keywords) भी चिन्हित करें ।
• आलेख का पाठः आलेख 4000-6000 शब्दों से अधिक न हो, जिसमें सारणी, ग्राफ भी सम्मिलित हैं।
• टाइपः कृपया अपना आलेख टाइप करके वर्ड और पीडीएफ दोनों ही फॉर्मेट में भेजे । टाइप के लिए हिंदी यूनिकोड का इस्तेमाल करें, अगर आपने हिंदी के किसी विशेष फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया हो तो फ़ॉन्ट भी साथ भेजे, इससे गलतियों की सम्भावना कम होगी, हस्तलिखित आलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
• अंकः सभी अंक रोमन टाइपफेस में लिखे। 1-9 तक के अंको को शब्दों में लिखें, बशर्ते कि वे किसी खास परिमाण को न सूचित करते हो जैसे 2 प्रतिशत या 2 किलोमीटर।
• टेबुल और ग्राफः टेबुल के लिए वर्ड में टेबुल बनाने की दी गई सुविधा का इस्तेमाल करें या उसे excel में बनाएं। हर ग्राफ की मूल एक्सेल कॉपी या जिस सॉफ़्टवेयर मैं उसे तैयार किया गया हो उसकी मूल प्रति अवश्य भेजे सभी टेबुल और ग्राफ को एक स्पष्ट संख्या और शीर्षक दें। आलेख के मूल पाठ में टेबुल और ग्राफ की संख्या का समुचित जगह पर उल्लेख (जैसे देखें टेबुल 1 या ग्राफ 1) अवश्य करें।
• चित्राः सभी चित्र का रिजोलुशन कम से कम 300 डीपीआई/1500 पिक्सेल होना चाहिए। अगर उसे कही और से लिया गया हो तो जरूरी अनुमति लेने की जिम्मेदारी लेखक की होगी।
• वर्तनीः किसी भी वर्तनी के लिए पहली और प्रमुख बात है एकरूपता। एक ही शब्द को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए। इसमें प्रचलन और तकनीकी सुविधा दोनों का ही ध्यान रखा जाना चाहिए।
• नासिक उच्चारण वाले शब्दों में आधा न् या म् की जगह बिंदी/अनुस्वार का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, संबंध के बजाय संबंध, सम्पूर्ण की जगह संपूर्ण लिखें।
• अनुनासिक उच्चारण वाले शब्दों में चन्द्रबिन्दु का प्रयोग करें। मसलन, वहाँ, आये , जाएंगे, महिलाएं, आदि-आदि। कई बार सिर्फ बिंदी के इस्तेमाल से अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, उदाहरण के लिए हंस और हँस।
• जहाँ संयुक्ताक्षरों मौजूद हों और प्रचलन में हों वहाँ उन संयुक्ताक्षरों का भरसक प्रयोग करें।
• महत्व और तत्व ही लिखें, महत्व या तत्व नहीं।
• जिस अक्षर के लिए हिंदी वर्णमाला में अलग अक्षर मौजूद हो, उसी अक्षर का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, गए गयी की जगह गए, गई लिखें।
• कई मामलों में दो शब्दों को पढ़ते समय मिलाकर पढ़ा जाता है उन्हें एक शब्द के रूप् में ही लिखें। उदाहरण के लिए, घरवाली, अखबारवाला, सब्जीवाली, गाँववाले, खासकर, इत्यादि।
• पर कई बार दो शब्दों को मिलाकर पढ़ते के बावजूद उन्हें जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है। खासकर सा या सी और जैसा या जैसी के मामले में। उदाहरण के लिए,एक-सा, बहुत-सी, भारत-जैसा, गांधी-जैसी, इत्यादि।
• अरबी या फारसी से लिए गए शब्दों में जहाँ मूल भाषा में नुक्ते का इस्तेमाल होता है। वहाँ नुक्ता जरूर लगाएं। ध्यान रहें कि क, ख, ग, ज, फ वाले शब्दों में नुक्ते का इस्तेमाल होताहै। मसलन, कलम, कानून, खत, ख्वाब, खैर, गलत, गैर इलरजत, इजाफा, फर्ज, सिर्फ।
•उद्धरणः पाठ के अंदर उद्धृत वाक्यांशों को दोहरे उद्धरण चिह्न (’ ’) के अंदर दें। अगर उद्धृत अंश दो-तीन वाक्यों से ज्यादा लंबा हो तो उसे अलग पैरा में दें। ऐसा उद्धृत पैराग्राफ अलग नजर आए इसके लिए उसके पहले बाद में एक लाइन का स्पेस दें और पूरा पैरा को इंडेंट करें और उसके टाइप साईज को छोटा रखें। उद्धृत अंश में लेखन की शैली और वर्तनी में कोई तबदीली या सुधार न करें ।
•पादटिप्पणी और हवाला (साईटेशन): सभी पादटिप्प्णियाँ और हवालों (साईटेशन) के लिए मूल पाठ में 1,2,3,4,..... सिलसिलेवार संख्या दे और आलेख के अंत में क्रम में दे। वेबसाईट के मामले में उस तारीख का भी जिक्र करे जब अपने उसे देखा हो। मसलन, पाठ 1, मनोरंजन महंती, 2002, पृष्ठ और हर हवाला के लिए पूरा संदर्भ आलेख के अंत में दें।
•सन्दर्भ: इस सूची में किसी भी संदर्भ का अनुवाद करके न लिखें, अथार्थ संदर्भो को उनकी मूल भाषा में रहने दें। यदि संदर्भ हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के हो तो पहले हिन्दी वाले संदर्भ लिखें तथा इन्हें हिन्दी वर्णमाला के अनुसार, और बाद में अंग्रेजी वाले संदर्भ को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूचीबद्ध करें ।
•ए.पी.ए. स्टाइल फोलो करें।
•मौलिकताः ध्यान रखें कि आलेख किसी अन्य जगह पहले प्रकाशित नहीं हुआ हो तथा न ही अन्य भाषा में प्रकाशित आलेख का अनुवाद हो। यानी आपका आलेख मौलिक रूप से लिखा गया हो।
•कोशिश होगी कि इसमें शामिल ज्यादातर आलेख मूल रूप से हिंदी में लिखे गए हो । लेखकों से अपेक्षा होगी कि वे दूसरे किसी लेखक के विचारों और रचनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे हर उद्धरण के लिए समुचित हवाला/संदर्भ देंगे ।अकादमिक जगत के भीतर बिना हवाला दिए नकल या दूसरों के लेखन और विचारों को अपना बताने (प्लेजियरिज्म) की बढ़ती प्रवृत्ति देखते हुए लेखकों का इस बारे मे विशेष ध्यान देना होगा ।
•समीक्षा और स्वीकृतिः प्रकाशन के लिए भेजी गयी रचनाओं पर अंतिम निर्णय लेने के पहले संपादक मडंल दो समीक्षकों की राय लेगा, अगर समीक्षक आलेख मे सुधार की माँग करें तो लेखक को उन पर गौर करना होगा।
•संपादन व सुधार का अंतिम अधिकार संपादकगण के पास सुरक्षित हैं।
•कापीराइटः प्रकाशन का कापीराइट लेखक के पास ही रहेगा पर हर रूप में उसका प्रकाशन का अधिकार आई आई पी ए के पास होगा। वे अपने प्रकाशित आलेख का उपयोग अपनी लिखी किताब या खुद संपादित किताब मे आभार और पूरे संदर्भ के साथ कर सकते हैं। किसी दूसरे द्वारा संपादित किताब में शामिल करने की स्वीकृति देने के पहले उन्हें आई आई पी ए से अनुमति लेनी होगी।